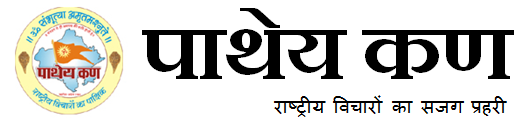इस्लाम में सुधार की गुंजाइश कितनी?

बलबीर पुंज
क्या लगभग डेढ़ सहस्राब्दी प्राचीन इस्लाम में सामाजिक सुधार संभव है? यह सवाल बार-बार उठता रहा है और कर्नाटक के हिजाब विवाद के चलते फिर से उठा है। मुस्लिम समाज का एक वर्ग अनुभव करता है कि ऐसा सम्भव नहीं है। ऐसा मानने वाले लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और स्वयं को ‘एक्स मुस्लिम’ घोषित कर रहे हैं। ऐसे मुस्लिम भारत में भी हैं। पिछले महीने ही इस्लाम छोड़ने वाले कुछ मुसलमानों ने ‘केरल के पूर्व मुस्लिम’ नामक एक संगठन बनाया है। देश में सार्वजनिक तौर पर ऐसा पहली बार हुआ। इस संगठन का उद्देश्य अपना मजहब त्यागने वाले मुस्लिमों को आर्थिक एवं भावनात्मक सहायता देना है। इस संस्था का दावा है कि उसके संपर्क में ऐसे सैकड़ों लोग हैं। परिवर्तन एक सार्वभौमिक-सतत प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी समाज में कालबाह्य हो चुकी परंपराओं-प्रथाओं को छोड़कर आगे बढ़ने का मानस होता है। किसी भी समाज में सुधार की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित दर्शन-मजहब आत्मसुधार तंत्र के प्रति कितना सहनशील है?
इस्लाम का जन्म हजरत मुहम्मद साहब को 610 में दैवीय ज्ञान प्राप्त होने के बाद हुआ। 632 में उनके न रहने के बाद उनके अनुचरों द्वारा इस ज्ञान को पवित्र कुरान के रूप में कलमबद्ध किया गया। चूंकि यह कार्य अरब में हुआ इसलिए मुस्लिम समाज की कई परंपराएं वहां के भूगोल और उसकी तत्कालीन संस्कृति से प्रभावित हैं। समय बीत जाने के बाद कई ऐसी परंपराएं आधुनिक जीवनशैली और मूल्यों से मेल नहीं खातीं। बहु-पत्नी चलन, तीन-तलाक, हिजाब-बुर्का आदि ऐसी ही प्रथाएं हैं। इन पर भारतीय मुस्लिम समाज ने न कभी गंभीर चर्चा की और न ही सुधार का कोई ठोस प्रयास। इसके विपरीत इन प्रथाओं को प्रोत्साहन दिया। इसी कारण देश के उन हिस्सों में भी हिजाब-बुर्का आदि का चलन बढ़ा है, जहां पहले नहीं था। इसकी तुलना में अन्य मतावलंबियों ने अपनी परंपराओं में समयानुकूल व्यापक स्वत: परिवर्तन किए या फिर उन्हें समाप्त कर दिया गया। आज सती प्रथा कोई मुद्दा नहीं। घूंघट प्रथा नगण्य है, कन्या-भ्रूण हत्या पर कानूनी रोक है तो दहेज और बाल विवाह के प्रति समाज जागरूक हो रहा है। इससे महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। हिंदू समाज सदियों से अस्पृश्यता से अभिशप्त रहा है, जिसके परिमार्जन हेतु समाज के भीतर से स्वर उठे। यह सिख गुरुओं की परंपरा से लेकर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, गांधीजी, आंबेडकर आदि के सतत प्रयासों का परिणाम है कि देश में आरक्षण-व्यवस्था लागू है और बौद्धिक स्तर पर छुआछूत का कोई भी समर्थन नहीं करता। यह सच है कि हिंदू समाज में अभी भी धरातल पर सामाजिक समरसता और समता अपूर्ण है, किंतु संतोष है कि इस दिशा में सुधार के प्रयास जारी हैं। इसके विपरीत मुस्लिम समाज में समयोचित बदलाव का अभाव है। यह स्थिति तब है, जब अन्य घोषित मुस्लिम देशों के साथ इस्लाम के जन्मस्थान सऊदी अरब के शाही परिवार, जिन्हें मक्का-मदीना का संरक्षक कहा जाता है, ने ‘विजन 2030’ नीति के अंतर्गत हाल के वर्षों में कई सामाजिक सुधार किए है।
सऊदी शासन की ओर से तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने, सिनेमाघरों पर दशकों से लगे प्रतिबंध हटाने, महिलाओं को वाहन चलाने और मक्का की तीर्थयात्रा सहित उन्हें अकेले यात्रा करने की अनुमति देने जैसे कई निर्णय लिए गए हैं। इन सुधारों का वैश्विक मुस्लिम समाज के भीतर से विरोध भी हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण सऊदी अरब की ओर से सदियों से इस्लाम के कठोर स्वरूप वहाबवाद का प्रचार-प्रसार करना रहा। इसे सऊदी अरब का दोहरा मापदंड ही कहेंगे कि एक ओर वह अपने समाज में सुधारों का नेतृत्व कर रहा है, तो दूसरी तरफ उस मदरसा शिक्षा पद्धति का मुख्य वित्तीय स्रोत भी बना हुआ है, जो संकुचित मानसिकता का निर्माण करती है। मध्यकालीन तालीम के चलते ही तालिबान सहित कई आतंकी संगठनों का जन्म हुआ है। काफिर-कुफ्र में पगी मजहबी खुराक का असर इतना गहरा होता है कि आधुनिक शिक्षा का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिविल इंजीनियर ओसामा बिन लादेन, न्यूरोसाइंस विशेषज्ञ आफिया सिद्दीकी, सर्जन अल जवाहिरी, पीएचडी अल बगदादी और लेक्चरर हाफिज सईद जैसे जिहादी इसके प्रमाण हैं।
इस्लाम छोड़ने वाले मुसलमानों को जो बात सर्वाधिक खटकती है, वह काफिर-कुफ्र अवधारणा ही है, जिसमें गैर-मुस्लिमों और उनकी संस्कृति-परंपरा के प्रति न केवल घृणा का भाव है, अपितु उन्हें मिटाने का मजहबी निश्चय भी। विवेकवान मुस्लिमों को यह प्रश्न परेशान करता है कि यदि इस्लाम शांति-भाईचारे और क्षमा-दया भाव युक्त मजहब है, तो काफिरों और शिर्क करने यानी अल्लाह के साथ अन्य देवी-देवताओं को मानने वालों के प्रति इतना शत्रुभाव क्यों?
हाल के समय में विश्व 9/11 आतंकी हमले सहित दर्जनों जिहादी घटनाओं से रूबरू हुआ है, किंतु भारत इसका दंश तब से झेल रहा है, जब 711-12 में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके जिहाद का सूत्रपात किया। इसके तीन सदी बाद महमूद गजनी ने भारत पर एक दर्जन से अधिक बार हमला करके सोमनाथ सहित असंख्य मंदिरों को ध्वस्त किया। इसी कारण वह अपने अनुचरों के बीच मूर्तिभंजक कहलाया। इसके बाद गोरी, खिलजी, तुगलक, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब, टीपू सुल्तान आदि ने भी काफिर-कुफ्र चिंतन से प्रेरित होकर यहां की बहुलतावादी सनातन संस्कृति के प्रतीकों को ध्वस्त किया और लाखों निरपराधों को या तो मौत के घाट उतारा या फिर उन्हें तलवार के बल पर इस्लाम अंगीकार करने हेतु विवश किया। इसी विभाजनकारी मजहबी चिंतन का मूर्त रूप पाकिस्तान है। भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी इन आक्रांताओं को अपना नायक मानता है। इस कारण भी कई मुस्लिम इस्लाम से विमुख हो रहे हैं। हाल में वसीम रिजवी के बाद मलयाली फिल्मों के निर्देशक अली अकबर ने इस्लाम का त्याग किया है।
क्या देश के मुसलमान आत्मचिंतन कर अपनी परंपराओं में सुधार किए बिना देश की प्रगति में शेष भारतीयों की भांति कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दे सकते हैं? यह सब तभी संभव होगा, जब भारतीय मुस्लिम समाज में भीतर से कालबाह्य रिवायतों को तोड़कर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो शायद तर्कशील और विवेकवान मुस्लिम इसी तरह इस्लाम से नाता तोड़ते रहेंगे।