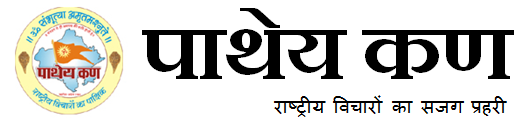अपनी जड़ों से जुड़ता भारत

बलबीर पुंज
 अपनी जड़ों से जुड़ता भारत
अपनी जड़ों से जुड़ता भारत
गत 26 जुलाई को असम के चराइदेव स्थित अहोम साम्राज्य के ‘मोइदम’ को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा सूचीबद्ध भारत का 43वां, तो देश में पूर्वोत्तर का प्रथम ‘विश्व धरोहर स्थल’ है। यह साम्राज्य असम में 13वीं से 19वीं शताब्दी के आरंभ तक अस्तित्व में रहा। क्या सुधी पाठक अहोम साम्राज्य के इतिहास को जानते हैं? यह विडंबना है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में दिल्ली सल्तनत (320 वर्ष), मुगल साम्राज्य क्रूर औरंगजेब की मौत तक (181 वर्ष) और ब्रितानी राज (190 वर्ष) का उल्लेख तो है, परंतु अहोम साम्राज्य का कार्यकाल 600 वर्षों से अधिक होने के बाद भी भारतीय पाठ्यक्रम से नदारद है। क्यों?
साधारण व्यक्तियों की तरह देश और समाज भी अपने अस्तित्व के प्रति ‘स्मृतिलोप’ रूपी रोग का शिकार होकर और बिना किसी दर्द को अनुभव किए समाप्त हो जाता है। आठवीं शताब्दी से भारत में इस्लामी आक्रांताओं (कासिम, गौरी, गजनवी, खिलजी, बाबर, टीपू सुल्तान सहित) के हमलों और मजहबी उन्माद के बाद वर्ष 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी सेना ने सिराज़ुद्दौला को हराकर ब्रिटिश राजकाज स्थापित किया था। इस्लामी कालखंड में भारतीय अस्मिता के प्रतीकों को जमींदोज किया गया, तो तलवार के बल पर हिंदू-बौद्ध-जैन-सिखों का जबरन मतांतरण। परंतु स्थानीय निवासियों ने कभी भी इस्लामी आक्रमणकारियों को स्वयं से श्रेष्ठ नहीं समझा और वे अपनी सांस्कृतिक पहचान-परंपराओं के प्रति गौरवान्वित रहे।
अंग्रेज होशियार और चालाक थे। उन्होंने स्थानीय भारतीयों को न केवल शारीरिक, बल्कि उन्हें उनकी मूल जड़ों से काटकर मानसिक तौर पर भी अपना गुलाम बनाना शुरू किया। जब वामपंथियों और जिहादियों की सहायता से भारत को तकसीम करके ब्रितानी 1947 में गए, तब तक वे भारत के सामूहिक मानस को क्षीण कर चुके थे। यह स्थिति तुरंत प्रभाव से बदलनी चाहिए थी और इसकी शुरुआत सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ प्रारंभ भी हुई। परंतु 30 जनवरी 1948 को गांधीजी की नृशंस हत्या और 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल के निधन के पश्चात इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर रोक लग गई और उस पर ‘सांप्रदायिकता’ का आवरण चढ़ा दिया गया।
ऐसा करने वालों में सबसे ऊपर स्वतंत्र और खंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू थे, जो अन्य ‘भारतीयों’ की भांति ब्रितानियों के ‘स्मृतिलोप अभियान’ का शिकार रहे। नेहरू मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित थे और वे लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले द्वारा स्थापित उस शिक्षण प्रणाली (1835-36) के अव्वल दर्जे वाले उत्पाद थे, जिसमें ‘रक्त-रंग से भारतीयों’ को ‘पसंद-नापसंद, विश्वास, नैतिकता और बुद्धि’ से अंग्रेज बनाने की नीति थी। विभाजन के बाद वामपंथियों ने मैकॉले-मानसपुत्रों के साथ मिलकर अपनी भारत-हिंदू विरोधी मानसिकता के अंतर्गत देश के वास्तविक इतिहास को और तहत-नहस कर दिया। दशकों बाद विशेषकर वर्ष 2014 के बाद इस स्थिति में स्वागत योग्य और चरणबद्ध वांछनीय सुधार हो रहा है।
हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम 95 वर्ष बाद बदलकर क्रमश: ‘गणतंत्र मंडप’ और ‘अशोक मंडप’ किया गया है। इससे पहले गत वर्षों में नए संसद भवन में प्राचीन चोल साम्राज्य के प्रतीक ‘सेंगोल’ (राजदंड) की स्थापना, काशी विश्वनाथ धाम का 350 वर्ष पश्चात विस्तारीकरण-पुनरोद्धार, न्यायिक निर्णय के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का पुनर्निर्माण, धारा 370-35ए का संवैधानिक क्षरण और प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को सिख पंथ के दसवें गुरु श्री गोबिंद सिंह साहिबजी के पुत्रों- साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान की याद में ‘वीर बाल दिवस’ के साथ प्रत्येक 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के रूप में मनाने आदि की घोषणा की गई थी।
इसी कड़ी में अहोम ‘मोइदम’ का यूनेस्को की ‘विश्व धरोहर सूची’ में शामिल होना अतुलनीय है। ये पिरामिड सरीखी अनूठी टीलेनुमा संरचनाएं हैं, जिनका प्रयोग छह सदियों तक ताई-अहोम वंश द्वारा अपने राजवंश के सदस्यों को उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ दफनाने के लिए किया जाता था। ‘मोइदम’ गुंबददार कक्ष (चौ-चाली) होते हैं, जो दो मंजिला होते हैं, जिनमें प्रवेश के लिए मेहराबदार मार्ग होता है और अर्धगोलाकार मिट्टी के टीलों के ऊपर ईंटों और मिट्टी की परतें बिछाई जाती हैं। ‘मोइदम’ दफन पद्धति अभी भी कुछ पुजारी समूहों और चाओ-डांग कबीले (शाही अंगरक्षक) द्वारा प्रचलित है।
मेरा वर्षों से मत रहा है कि सिख पंथ के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर साहिबजी के बलिदान (नवंबर 1675) को ‘राष्ट्रीय कृतज्ञता दिवस’ के रूप में मनाना चाहिए। वे ‘हिंद की चादर’ यूं ही नहीं कहलाए। गुरु साहिब का बलिदान ‘धर्म’ की रक्षा के लिए था। उन्होंने जीवनभर उस परंपरा का अनुसरण किया, जो किसी एक क्षेत्र या समुदाय के लिए समर्पित नहीं था। जिनकी सुरक्षा करते हुए गुरु साहिब ने सर्वोत्तम बलिदान दिया, वह पंजाब के नहीं, कश्मीर के थे, हिंदू थे। जैसे कश्मीर आज इस्लामी आतंकवाद का शिकार है, ठीक उसी तरह के मजहबी संकट से गुरु साहिब भी दो-चार थे। जब कश्मीर में जिहादी दंश झेल रहे हिंदुओं की फरियाद लेकर गुरु साहिब क्रूर औरंगेजब के पास पहुंचे, तब उन्हें इस्लाम स्वीकार करने या मौत चुनने का विकल्प दिया गया। गुरु साहिब ने अपने तीनों अनुयायियों की नृशंस हत्या के बाद भी दृढ़ होकर अपना शीश कटाना स्वीकार किया। इस घटना का वर्णन ‘बचित्तर नाटक’ में श्री गुरु गोबिंद सिंहजी ने कुछ इस प्रकार किया था- “तिलक जंजू राखा प्रभ ताका… सीसु दीआ परु सी न उचरी॥ धरम हेत साका जिनि कीआ॥ सीसु दीआ परु सिररु न दीआ॥” अर्थात— हिंदुओं के तिलक और जनेऊ की रक्षा हेतु गुरु तेग बहादुरजी ने अपने शीश का त्याग कर दिया, किंतु धर्म नहीं छोड़ा।
यह विडंबना है कि जिस पवित्र सिख गुरु परंपरा के चलते महाराजा रणजीत सिंह (1780-1839) के कालखंड तक हिंदू-सिख के संबंध नाखून और मांस जैसे थे, उसे भी ब्रितानियों ने मैक्स आर्थर मैकॉलीफ के माध्यम से चीरने का प्रयास किया था। यह घाव अभी पूरी तरह भरा नहीं है। इसका पूर्ण इलाज तभी संभव है, जब हर भारतीय सभी सिख गुरुओं के जीवन को जाने, समझे और उनके द्वारा स्थापित जीवनमूल्यों को अंगीकार करने का प्रयास करें।
(हाल ही में लेखक की ‘ट्रिस्ट विद अयोध्या: डिकॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया’ पुस्तक प्रकाशित हुई है)