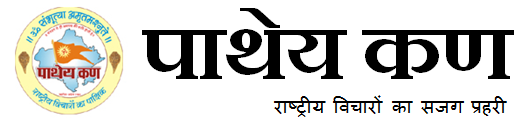देशज चिंतन शैली में ही निहित है भारत की सभी समस्याओं का समाधान

रवि प्रकाश

समस्या चाहे जैसी भी हो, चिंतन कर उसका समाधान निकाला जा सकता है। समाधान क्या निकलेगा, वह समाधान कारगर होगा कि नहीं, समस्याओं को सुलझाने में सफलता मिलेगी या नहीं, यह आपकी चिंतन शैली पर निर्भर करता है। आपकी चिंतन शैली आपकी मनोदशा, आपके आचार-व्यवहार और कुछ हद तक आहार पर भी निर्भर करती है। हममें से अधिकांश लोगों ने देखा होगा कि कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के कमरे बड़े, कनिष्ठ अधिकारियों के कमरे छोटे होते हैं और सामान्य कर्मचारियों को अलग एक साथ बैठना पड़ता है। कंपनी चाहे तो सबको एक साथ बैठा सकती है। किसी को कोई समस्या भी नहीं होगी। मगर ऐसा नहीं होता। इसका कारण यह होता है कि जिसके पास जितना बड़ा दायित्व होता है, उसके सोचने का दायरा उतना बड़ा होता है। बड़ा सोचने के लिए बड़ी और खुली जगह में बैठना आवश्यक होता है। आप छोटी जगह में बैठकर बड़ा सोच ही नहीं सकते हैं। विश्वास न हो तो आजमा कर देख लीजिए।
स्थान के साथ-साथ चिंतन शैली की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चिंतन शैली दो प्रकार की होती है – एक देशज और दूसरा आयातित। देशज चिंतन शैली में किसी भी समस्या का समाधान जमीन, जल, जंगल, जानवर, कृषि, गोपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय को ध्यान में रखकर किया जाता है। जबकि आयातित सोच में इनमें से किसी भी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि उस सोच से विकसित उपाय कभी स्थायी समाधान नहीं दे पाते हैं। स्वतंत्रता के 73 वर्षों के बाद भी हम यदि विकासशील देश की पंक्ति में गिने जाते हैं तो इसके लिए आयातित सोच ही दोषी है। यह आयातित सोच का ही दुष्परिणाम था कि न तो हम अपनी पुरानी व्यवस्था को लागू कर पाए और न ही पूरी तरह से विदेशी व्यवस्था को क्रियान्वित कर पाए। यह आयातित सोच का ही परिणाम है कि हमारे देश की सत्ता के चार महत्वपूर्ण स्तंभ धर्मसत्ता, समाजसत्ता, राजसत्ता, अर्थसत्ता को हमने त्याग दिया। नतीजा यह हुआ कि न हमें माया मिली न राम। हमने अपने देश के आत्मनिर्भर गाँवों को गोबर बना दिया और शहरों को इस लायक बना नहीं पाए कि उन्हें केन्द्र में रखकर देश और देशवासियों के भविष्य को सँवारा जा सके। यह आयातित सोच का ही प्रभाव था कि भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया और इन नापाक प्रयासों को सफलता भी मिली। जिनकी आयु आज साठ साल के आस-पास होगी उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि हमारे देश में बना सिल्क कपड़े का एक थान एक अंगूठी में इस पार से उस पार हो जाता था। यह सुनी सुनाई बात नहीं है। इन दिनों बच्चों को पढ़ने के लिए जो कुछ भी उपलब्ध कराया जा रहा है, उनमें इन बातों का जिक्र नहीं है। हम कृषि प्रधान देश नहीं, बल्कि कुटीर उद्योग प्रधान देश हुआ करते थे। यह दूषित मानसिकता और आयातित सोच का ही नतीजा था कि भारत कुटीर उद्योग प्रधान से कृषि प्रधान देश बन गया क्योंकि हमारा नेतृत्व तय करने में असमर्थ था कि हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। उसके पास चिंतन का अभाव था। आयातित सोच में हुई परवरिश में अपने देश की मिट्टी के लिए जगह नहीं थी।
जब हम वर्ष 1945 से 1955 तक के कालखण्ड पर नजर डालते हैं, तब हमें कुछ बातें साफ दिखाई देती हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद विश्व दो टुकड़ों में बँटा था। एक तरफ अमरीका और इंग्लैंड था तो दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली। आजादी के बाद हमारा नेतृत्व राजनैतिक रूप से इंग्लैंड के लोकतांत्रिक ढाँचे और व्यवस्था से प्रभावित था तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से उसे रूस आकर्षित कर रहा था। एक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के घालमेल के दुष्परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। लगभग तीन दशक तक यह घालमेल चलता रहा और जब हमारी नींद टूटी तो हम बाजारवाद का अनुसरण करने के लिए अमरीका की गोद में बैठ चुके थे।
जो होना था हो चुका है। अब वह समय आ गया है, जब हम अपनी हर तरह की व्यवस्था को नई सोच, नई दिशा के साथ शुरू कर सकते हैं। कोरोना के संक्रमण से वैश्विक व्यवस्था चरमरा गई है। हम यदि पुराने रास्ते पर चलते हुये इस ठीक करने का प्रयास करेंगे तो यह कभी ठीक नहीं होगा। हमें इस अवसर को पहचानना चाहिए और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की दिशा में प्रयास कर नये भारत में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।
नये भारत का ताना बाना धर्मसत्ता, समाजसत्ता, राजसत्ता, अर्थसत्ता को केन्द्र में रखकर तैयार किये जाने की आवश्यकता है। हमारे देश का युवा वर्ग दिग्भ्रमित है। अब तक उसे सिर्फ यही समझाया गया है कि सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानते हैं और इसी सोच को ध्यान में रखकर हमने शिक्षा व्यवस्था भी तैयार की थी। जिस शिक्षा व्यवस्था को हम इतने सालों से ढोते चले आ रहे हैं, उनमें कौशल विकास का कोई स्थान भी नहीं है। हुनरमंद हाथों को नौकरी की दरकार नहीं होती है। वह अपनी व्यवस्था खुद करने में सक्षम होता है। इससे स्व-रोजगार का विकास होता है। अंग्रेजों से हमें 73 वर्ष पहले आजादी मिल चुकी है, अब अंग्रेजियत से मुक्त होने का समय आ गया है। अब हमें अपनी नीतियां जमीन, जल, जंगल, जानवर, कृषि, गोपालन, शिक्षा (विद्या), स्वास्थ्य और न्याय को केन्द्र में रखकर बनानी होंगी। हम यह मानते और जानते हैं कि 70 साल का जो कचरा जमा है, वह एक दिन में साफ नहीं हो सकता है। लेकिन अब उसे धीरे-धीरे साफ करना शुरू कर देना चाहिए। इस कचरे में कुछ अच्छाइयाँ भी दबी होंगी। उन अच्छाइयों को कचरे के साथ फेंक नहीं देना है, बल्कि नव-निर्माण में उपयुक्त स्थान पर उसका उपयोग करना है। हम सभी जानते हैं कि कमजोर आधारशिला पर मजबूत इमारत की नींव नहीं रखी जा सकती है। इसकी जड़ में स्वदेशी की अवधारणा होनी चाहिए। प्रकृति के अनुकूल संस्कृति की आधारशिला रखी जानी चाहिए। इस नई अवधारणा में प्रकृति को केन्द्र में रखा जाना चाहिए। एकात्मता, समता, संपन्नता के साथ विज्ञान और अध्यात्म का संगम होना चाहिए।
हमारी सामाजिक सत्ता का ताना-बाना तो अंग्रेजों ने ही छिन्न-भिन्न कर दिया था। जो बचा था, उसे हमारे नेतृत्व ने जमींदोज कर दिया। बाजारवादी व्यवस्था की जकड़न से परिवार की व्यवस्था टूट गई। पुरखों से जो एक साथ रहते थे, वे एक-एक कमरे में अलग-अलग रहने लगे। सामूहिक रसोई का ताना-बाना बिखर गया। जब खाना अलग-अलग पकने लगे तो उसका असर लोगों की मानसिकता पर भी दिखने लगा। एक ही खून की सोच में भिन्नता आ गई। यह भिन्नता समाज के लिए घातक बन गई। अकेलापन, हिंसक मनोभाव, आत्महत्या, इस अप्राकृतिक विकास-व्यवस्था के दुष्परिणाम हैं। इस तरह के अप्राकृतिक विकास में बाजारवाद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाज में पारिवारिक व्यवस्था के विघटन और बचत की आदत को छुड़ाने में बाजारवादी व्यवस्था की भूमिका बहुत बड़ी है। इस विदेशी विकास मे समाज की हजारों साल की वर्जनाएँ टूट रही है, उन्मुक्त पशुवत् उपभोग को खुशहाली के रूप में चित्रित किया जा रहा है। प्रकृति का विध्वंस, गैर-बराबरी, बेवजह स्लमीकरण आदि विदेशी विकास के लक्षण है।
वैश्वीकरण की जिस विचारहीन दौड़ में हम दौड़ते रहे हैं, उसके परिणाम देश के लिए हितकर नहीं रहे। ग्रामीण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, लेकिन इसका लाभ किसी को नहीं हुआ। गांव बच्चों और बूढ़ों का केन्द्र बनकर रह गया। युवाओं का पलायन हो गया। रोजगार की तलाश में वे या तो शहर पहुंच गए या फिर समृद्ध राज्यों में मजदूरी करने चले गए। युवाओं के पलायन से गांव की गरीबी घट गई हो, ऐसा भी नहीं हुआ। वहां भी दो वर्ग बन गए। एक पैसे वालों का और दूसरा गरीबों का। दो वर्गों के बन जाने से गांव की एकता और समरसता छिन्न-भिन्न हो गई।
अर्थसत्ता तो पूरी तरह चरमरा चुकी है। विश्व का कोई भी देश अपने देश की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए अपने व्यवस्था तैयार करता है। हमने अपनी सुविधाओं और व्यवस्थाओं को तुच्छ समझा। हम अपनी विशेषता, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था व कुटीर उद्योग को दकियानूसी और पिछड़ा समझा और उसकी उपेक्षा कर उसे नष्ट करने का प्रयास शुरू कर दिया। वैश्वीकरण की दौड़ में पहले हमने अपने कुटीर उद्योग नष्ट किए और बाद में आयात को खोलकर उद्योगों को बंदी के कगार पर पहुंचा दिया। प्रकृति ने हमें इतना कुछ दे रखा है कि हम समझ हीं नहीं पाते कि उसका उपयोग कैसे करें। अपने देश में 127 पारिस्थितिकी कृषि-जलवायु क्षेत्र (इको एग्री क्लाइमेट जोन) हैं। यदि इस बात को हम समझ लेते तो हमें आज किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। एग्री क्लाइमेट जोन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यदि हमने अपनी खेती के तरीके को विकसित किया होता तो हमें किसी से कुछ माँगने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक होता। हम लेने नहीं बल्कि देने की स्थिति में होते।
विकास की हर अवधारणा के पीछे गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य बताया जाता रहा। मगर परिणाम यह हुआ कि वर्ष 1995 की तुलना में 15 वर्ष बाद अमीर और गरीब के बीच की विषमता बढ़ गई। 30 वर्ष पूर्व दुनिया की 70% संपदा 30% लोगों के हाथ में थी। अब 80% संपदा 20% लोगों के हाथ आई। भारत में ऊपरी 1% आबादी के पास देश के 57% संसाधन आ गए।
अर्थसत्ता की बिगड़ी व्यवस्था कैसे ठीक होगी, यह तय करना तो राज्यसत्ता के दायरे में आता है। यदि एक बार फिर से हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की अंधेरी सुरंग में दौड़ने के लिए तैयार होंगे तो यह हमारी अभी तक की सबसे बड़ी भूल होगी। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जल, जमीन, कुटीर उद्योग और पशु पालन को प्राथमिकता देनी चाहिए। हो सकता है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में कुछ समय लगे मगर जब वह लौटेगी तो मजबूत बनकर लौटेगी और इसे लौटाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। यदि भारत को आगे बढ़ना है, अपने प्रतिद्वंद्वी पड़ोसियों से मजबूत बनाना है तो इसे अपनी भूमि, अपने जंगल, अपने पहाड़, अपने पशु-पक्षी और वनस्पतियों से प्रेम और उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही भारत को अपने लोगों की चिंतन-धारा को उन विस्मृत, सुसुप्त धारा से जोड़ना होगा, जिसके वेग से भारत की ऊर्जा और रश्मि-किरणें सम्पूर्ण विश्व में प्रवाहित होतीं थीं। कतिपय तथाकथित स्वयंभू और स्वघोषित आधुनिक लोगों को वह धारा राष्ट्रवादी वर्चस्व का पर्याय लग सकती है, किन्तु वह धारा ही वह मूल है। जिससे सम्बन्ध विच्छेद होने से भारत अपनी अस्मिता और ऊर्जा संरक्षित नहीं रख सकता। उसी धारा से मुँह मोड़ने और विजातीय बीजों को भारतीय मिट्टी में प्रस्फुटित करने के हठ ने हमसे वह सब छीन लिया, जिसके सहारे हम अभाव में भी प्रभाव के साथ जीवन के यौवन का यशोगान कर लेते थे। आज वह पीढ़ी ज़िंदा है, जिसने गाँवों में आनंद और संकट, दोनों क्षणों में पूरे गाँव को एक परिवार के रूप में एकत्रित होते देखा है। वह भारतीयता की आत्मा है। यही हमारी मूल पहचान है, जो कहीं खोती जा रही है। हमारी जीवन प्रत्याशा तो बढ़ी, लेकिन जीवन अपनी गहराई से निकल कहीं उथली सतह पर आ गया। हमारे बटुए तो बड़े हुए, लेकिन हमारा मन छोटा होता गया। हम विद्यावान के बदले शिक्षित हो गए, तो “विद्या ददाति विनयम” भी कहीं गुम हो गया।
प्रकृति के नैसर्गिक अनुभूतियों से दूर आज का भारतीय मानस अगर अपनी जड़ों की और नहीं लौटा तो वह दुर्बल हो जाएगा। भारत की आत्मा प्रकृति के साथ सहचर्य में वास करती रही है। कहीं से कोई सिद्धांत उड़ चला – प्रकृति का दोहन और हम चल पड़े इस दोहन के पीछे। परिणाम ! पिछले 50 वर्षों में 80% जैव-विविधता समाप्त हो गई। जीवन दूभर हो गया। जीवन की इस दुर्वहता को समाप्त करने के लिए भविष्य के निर्माण को एक बार पुनः अतीत की बुनियाद से आरम्भ करने की आवश्यकता है. और यह आवश्यकता सामूहिक इच्छाशक्ति से ही पूरी हो सकती है. इस दिशा में सभी को साथ मिलकर चलना होता – सरकार को भी, समाज को भी, जनता को भी !
(लेखक भारत विकास परिषद के पश्चिमी क्षेत्र के रीजनल सेक्रेटरी (सेवा) हैं)