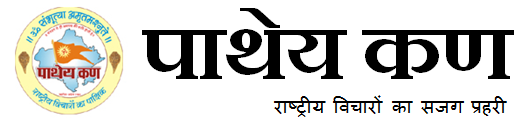पाकिस्तान का टूटता तारा बलूचिस्तान (भाग 2)

प्रशांत पोळ
 पाकिस्तान का टूटता तारा बलूचिस्तान (भाग 2)
पाकिस्तान का टूटता तारा बलूचिस्तान (भाग 2)
बलूचिस्तान को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। विस्तीर्ण भू प्रदेश है, जिसमें रेगिस्तान है, जंगल हैं, दर्रे हैं, समंदर है, बर्फ है…! सब कुछ है। पाकिस्तान का आधे से थोड़ा कम हिस्सा याने बलूचिस्तान। लेकिन जनसंख्या के मामले में बहुत कम। पाकिस्तान का हर पांचवां आदमी बलूचिस्तान से होता है।
राजधानी क्वेट्टा, बेहद खूबसूरत शहर है। यह फलों का शहर है। शहर के चारों ओर फलों के बगीचे। भरपूर फल, सूखे मेवों से सजे बाजार और शाम की ठंडी हवाएं। किसी समय क्वेट्टा ‘छोटा पेरिस’ कहलाता था। लेकिन आज नहीं। आज क्वेट्टा, बम धमाकों से पहचाना जाता है।
पाकिस्तान को जो 990 किलोमीटर का सागर किनारा मिला हुआ है, वह दो राज्यों के पास है – सिंध (270 किलोमीटर) और बलूचिस्तान (मकरान ७२० किलोमीटर)। सिंध के पास कराची जैसा विशाल बंदरगाह है, तो बलूचिस्तान के पास, अभी – अभी चीन का बनाया हुआ अत्याधुनिक ग्वादर बंदरगाह है।
कराची से ईरान की तरफ यदि हम अरेबियन समुद्र के किनारे से, ओमान की खाड़ी में बढ़ते जाते हैं, तो बलूचिस्तान राज्य के सोनमियानी, ओरमारा, कालमत, पासनी ऐसे बंदरगाह आते हैं। लेकिन ईरान की सीमा के पास, ओमान के सामने बना ग्वादर बंदरगाह भव्यतम है। यह बंदरगाह याने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के रास्ते में खड़ी एक दीवार है…! चूंकि ग्वादर बंदरगाह का विकास चीन ने किया है, इसलिए इस बंदरगाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी चीन ने ली है। अगले चालीस वर्षों का ग्वादर का स्वामित्व (लीज) चीन के पास है। इसलिए चीन वहाँ अपनी नौसेना का अड्डा बना रहा है। इसी संदर्भ में दो महीने पहले, पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख, अमजद खान नियाजी और चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफ़ू के बीच रक्षा सहयोग पर सहमति बनी है। इसका अर्थ स्पष्ट है – ग्वादर और उसके आस पास के समुद्री क्षेत्र में चीनी फौजों की संख्या बढ़ने जा रही है। बलोचिस्तान के लोगों को यह सब पसंद नहीं है। परतंत्रता की जंजीरें जकड़ती जा रही हैं, ऐसा उन्हें लगता है।
ग्वादर बंदरगाह चीन की महत्वाकांक्षी सीपीईसी (China Pakistan Economic Corridor) परियोजना का हिस्सा है। ग्वादर को चीन के शिंजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए चीन, २४४२ किलोमीटर का आधुनिक रास्ता, पाकिस्तान में बना रहा है। चीन को लगने वाला तेल (पेट्रोलियम पदार्थ) और मछली, चीन ग्वादर से, सड़क मार्ग से, अपने देश तक लेकर जाना चाहता है। किन्तु बलोच लोगों के विरोध से और पाकिस्तानी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार से यह रास्ता पूरा नहीं बन पाया है। बलूचिस्तान के नागरिक इस परियोजना और चीनी नागरिकों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।
बलूचिस्तान किसी जमाने में विशाल भारत का हिस्सा था। इससे पहले हमने देखा है कि समूचा बलूचिस्तान, उन दिनों गांधार महाजनपद का हिस्सा था। किन्तु बलूचिस्तान के भारत से आज भी काफी निकट के संबंध हैं, रिश्ते हैं। एक संबंध, हजारों वर्ष पुराने रिश्तों की कड़ियाँ जोड़ता है। बलूचिस्तान के कलात में जो ब्राहुई भाषा बोली जाती है, वह अपने दक्षिण भारत की द्रविड़ियन भाषा का ही एक प्रकार है। तमिल, कन्नड़ और तेलगु से बहुत कुछ मिलती – जुलती है। इस भाषा के अनेक शब्द तमिल, कन्नड़ भाषाओं से लिए गए हैं। त्रिचनापल्ली के एक मित्र ने बताया कि उसने जब यह ब्राहुई भाषा की यू-ट्यूब चैनल देखी, तो उसे बहुत कुछ समझ में आया। कुछ समान शब्द –
तुम (You) – नी
आंखें (Eye) – कन
थूकना (Spit) – थुप्पू
पुत्र – लड़का (Son) – मखम यार
रोबर्ट कॉलवेल्ड (1891) ने इन दोनों भाषाओं की समानता पर बहुत अध्ययन किया है। उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि ब्राहुई भाषा में तमिल एवं कन्नड़ के अनेक शब्द हैं। साथ ही दोनों भाषाओं की शैली भी एक जैसी है। किन्तु कालांतर से ब्राहुई भाषा, फारसी लिपि में लिखी जाने लगी है।
बलूचिस्तान से भारत का दूसरा रिश्ता पिछले ढाई सौ – पौने तीन सौ वर्ष पुराना है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पराजित होने के बाद, मराठा सेना के लगभग बीस – पच्चीस हजार सैनिकों और महिलाओं को अब्दाली अपने साथ ले गया। रास्ते में पंजाब में सिख सेनानियों ने कुछ महिलाओं को तो छुड़वा लिया, किन्तु बाकी मराठों को बंदी बनाकर ले कर जाने में वह सफल रहा। अब्दाली का रास्ता बलूचिस्तान होकर जाता था। पानीपत के युद्ध में, लूट और खजाना मिलने की आशा में, उसे बलूच सरदारों ने काफी सहयोग दिया था। इस पानीपत के युद्ध में मराठे हारे तो अवश्य, किन्तु उन्होंने इतना जबरदस्त संघर्ष किया, कि अब्दाली के हाथ कुछ अधिक न लग सका। इसलिए अब्दाली ने खजाने के बदले, सभी बीस – पच्चीस हजार मराठे, गुलाम के रूप में, बलूच सरदारों को दे दिये। वस्तुतः पानीपत के युद्ध में अब्दाली की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो जीत अवश्य गया था, लेकिन उसकी कमर टूट गई थी। (इसीलिए, अब्दाली के बाद, किसी ने भी खैबर के दर्रे से भारत पर आक्रमण का साहस नहीं किया)। अब्दाली को इन बीस – पच्चीस हजार मराठा कैदियों को ढो कर अफगानिस्तान ले जाना संभव ही नहीं था।
वे 20 – 25 हजार मराठा सैनिक वहीं बस गए। पहले बुगती और मर्री समुदाय के नौकर के रूप में रहने वाले मराठा सैनिक, बाद में अपने बलबूते पर उन्हीं समुदायों का हिस्सा बन गए।
आज लगभग 25 लाख मराठा, बुगती और मर्री समुदाय में हैं। ये सब मुस्लिम हो गए हैं, लेकिन अपना मूलाधार नहीं भूले हैं। ये सब अपने नाम के आगे ‘मराठा’ लिखते हैं। उनके बहुत से रीति रिवाज, विवाह पद्धति, महाराष्ट्र की परंपरा से मिलते जुलते हैं। उनका एक संगठन है – ‘मरहट्टा कौमी इत्तेहाद ऑफ बलोचिस्तान’ (Marhtta Qaumii Ittehad of Balochistan)। इस समुदाय के प्रमुख व्यक्ति हैं – वडेरा दीन मुहम्मद मराठा (जमींदार दीन मुहम्मद मराठा)। डेरा बुगती और सुई हिन्दू समुदाय, इन वडेरा दीन मुहम्मद साहब को बहुत सम्मान देता है।
इन सब की स्वाभाविक कड़ी, पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती। बहुत पहले से बलूचिस्तान अलग था। इसीलिए आज भी इनको पाकिस्तान के साथ रहना नहीं है। और भी कारण हैं।
बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। विशेषतः प्राकृतिक गैस बड़े पैमाने पर निकलती है, जो पाकिस्तान सरकार की आमदनी का बड़ा हिस्सा है। लेकिन जहां से यह गैस निकलता है, उस बलूचिस्तान के पास उस आमदनी का अत्यंत नगण्य छोटा सा हिस्सा आता है। इस कारण बलूचिस्तान प्रांत में विकास का चित्र कहीं दिखता नहीं है। अभी कुछ वर्षों में ग्वादर बंदरगाह पर जाने वाला जो एक्सप्रेस-वे चीन ने बनाया है, उसे छोड़ा दिया जाए, तो बलूचिस्तान में आज भी आधारभूत संरचना (इनफ्रास्ट्रक्चर) की भारी कमी है, और इसीलिए बलूच लोगों ने, 27 मार्च 1948 को, जब पाकिस्तान ने उसे बलात अपने कब्जे में लिया, तब से पाकिस्तान के विरोध में विद्रोह का स्वर बुलंद किया है।
(क्रमशः)