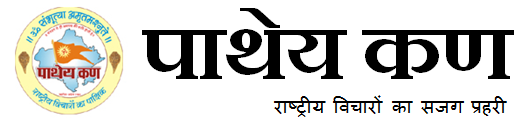बसंतोत्सव एवं महाकुम्भः वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व

डॉ. शिवा शर्मा
 बसंतोत्सव एवं महाकुम्भः वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व
बसंतोत्सव एवं महाकुम्भः वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व
बसंत प्रकृति एवं मानव मन के संयोग का सुंदर पर्व है। प्रकृति अपने समस्त श्रृंगार के साथ बसंत का अभिनंदन करती है। सुरमित आम के बौर और कोयल की कूक से बसंत के आगमन का संदेश प्रसारित होता है। इस संदेश से मानव मन भी पुलकित एवं उल्लासित हो उठता है। बसंत मन में नव उमंग व हृदय में सजल भाव को जगाता है। नई आशाओं एवं कामनाओं को जन्म देता है। संभवतः इन्हीं सब कामनाओं को परिष्कृत और उदत्त करने के लिए सरस्वती पूजन की परंपरा प्रचलित हुई है।
पौराणिक कथा कहती है कि हिन्दू कैलंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्माजी ने अनुभव किया कि जीवों के सृजन के बाद भी चारों ओर मौन छाया रहता है। उन्होंने विष्णुजी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। छह भुजाओं वाली इस शक्ति के एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में पुष्प, तीसरे और चौथे हाथ में कमंडल और बाकी दो हाथों में वीणा और माला थी। ब्रह्माजी ने देवी सरस्वती के प्रादुर्भाव के बाद उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुरनाद किया, चारों और ज्ञान और उत्सव का वातावरण हो गया, वेदमंत्र गूंज उठे। ऋषियों की अंतःचेतना उन स्वरों को सुनकर झूम उठी। ज्ञान की जो लहरियां व्याप्त हुई, उनको ऋषिचेतना ने संचित कर लिया। इसी दिन को बंसत पंचमी के रूप में मनाया जाता है।
बसंत पंचमी पर्व का धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व :
सादगी और निर्मलता को दर्शाता है पीला रंग, हर रंग की अपनी विशेषता है जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। हिन्दू धर्म में पीले रंग को शुभ माना गया है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। यह शुभत्व, सादगी और निर्मलता को भी दर्शाता है।
आत्मा से जोड़ने वाला रंगः
फेंगशुई ने भी इसे आत्मिक रंग अर्थात आत्मा वा अध्यात्म से जोड़ने वाला रंग बताया है। फेंगशुई के सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित हैं। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का है यानी यह ऊष्मा शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग हमें तारतम्यता, संतुलन, पूर्णता और एकाग्रता प्रदान करता है।
सक्रिय होता है दिमागः
मान्यता है कि यह रंग डिप्रेशन दूर करने में कारगर है। यह उत्साह बढ़ाता है और दिमाग सक्रिय करता है। नतीजतन दिमांग में उठने वाली तरंगें खुशी का अहसास कराती हैं। हम पीले परिधान पहनते हैं तो सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से दिमाग पर असर डालती हैं।
बसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशा का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, व्यंजन बनाते हैं।
कालिदास ऋतुसंहार में कहते हैं-
डुमा सपुष्याः सलिलं सपदम स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः
सुखाः प्रदोषाः दिवसाश्च रम्याः, सर्व प्रिये चारुतरं वसन्ते ।।
वापीजलानां मणिमेखलानां शशाङ्ङ्कभासां प्रमदाजनानाम् । चूत्रुमाणां कुसुमान्वितानां ददाति सौभाग्यमयं वसंतः ।।
अर्थात्
ऐसी मनभावन ऋतु आई, वृक्षों की हर डाली डाली पुष्पित है प्रमुदित है मन में प्रफुल्लित है पद्म हर एक जलाशय में और प्रवाहित है सुगन्धित पवन हर दिशा दिशा में दिवस सुरम्य। सुखकर सन्ध्या ऐसा चास्तर है वसन्त तभी तो प्रिय है सभी को..हर और एक आकर्षण / एक सम्मोहन
पहल से भी कहीं अधिक जलाशयों के वहट्टे हुए जल को / मणिखचित मेखलाओं को कंगनों को चन्द्रमा की चन्द्रिका को सुकुमारियों की सुकुमारता को और पुष्याभूषणों से आभूषित आम्रवृक्षों को दिया है दान सौन्दर्य का / सौभाग्य का इसी वसन्त ने तो…
तभी तो है इतना मोहक और आकर्षक…
वर्तमान में प्रयागराज में चल रहा कुम्भ मेला कई शताब्दियों से मनाया जाता है। कुम्भ मेला बेहद पवित्र और धार्मिक मेला है और भारत के साधुओं और संतों के लिए विशेष महत्व रखता है। वे वास्तव में पवित्र नदी के जल में स्नान करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। विभिन्न अखाड़ों से संबंधित साधु-संन्यासी बड़ी संख्या में यहां आते हैं। घाटों की ओर जाते समय जब वे भजन, प्रार्थना और मंत्र गाते हैं, तो उनका जुलूस देखने लायक होता है।
कुम्म मूल शब्द कुम्भक (अमृत का पवित्र घड़ा) से आया है। ऋग्वेद में कुम्भ और उससे जुड़े स्नान का उल्लेख है। इसमें इस अवधि के दौरान संगम में स्नान करने से लाम, नकारात्मक प्रभावों के उन्मूलन तथा मन और आत्मा के कायाकल्प की बात कही गई है। अथर्वेद और यजुर्वेद में भी कुम्भ के लिए प्रार्थना लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन से निकले अमृत के पवित्र घड़े (कुंभ) को लेकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर कुम्भ को लालची राक्षसों के चंगुल से छुड़ाया था। जब वह इसे लेकर स्वर्ग की ओर लेकर मागे तो अमृत की कुछ बूंदे चार पवित्र स्थलों पर गिरीं जिन्हें हम आज हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इन्हें चार स्थलों पर प्रत्येक तीन वर्ष पर बारी-बारी से कुम्भ मेले का आयोजन किया जाता है।
महाकुम्भ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। बल्कि यह प्राचीन भारत की गहन वैज्ञानिक और खगोलीय समझ का प्रतीक है। यह मेला हमें सिखाता है कि आस्था और विज्ञान के बीच कोई विभाजन नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर मानवता के लिए मार्गदर्शक बनते हैं।
विज्ञान और अध्यात्म का संगम :
ग्रहों की स्थिति का न केवल आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से यह पृथ्वी और मानव पर पड़ने वाले प्रभावों को भी दर्शाती है। गुरु, सूर्य और चंद्रमा का विशेष संयोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। इन खगोलीय संयोगों के दौरान कुम्भ में स्नान का महत्व अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय है।
कुम्भ का जियोग्राफिकल महत्व :
कुम्भ मेला आयोजन स्थलों का चयन भू-चुंबकीय ऊर्जा के आधार पर किया गया है। ये स्थान, विशेषकर नदी संगम क्षेत्र, आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल माने गए हैं। प्राचीन ऋषियों ने इन स्थानों पर ध्यान, योग और आत्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त ऊर्जा प्रवाह का अनुभव किया और इन्हें पवित्र घोषित किया था।