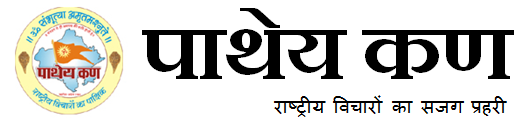मुस्लिमों का गैर मुस्लिमों के साथ ही अपने मुस्लिम बंधुओं से भी सतत टकराव क्यों?

बलबीर पुंज
 मुस्लिमों का गैर मुस्लिमों के साथ ही अपने मुस्लिम बंधुओं से भी सतत टकराव क्यों?
मुस्लिमों का गैर मुस्लिमों के साथ ही अपने मुस्लिम बंधुओं से भी सतत टकराव क्यों?
विश्वभर में दशकों से इस्लाम अलग-अलग कारणों से चर्चा में है। दुनिया में 55 से अधिक या तो घोषित इस्लामी गणराज्य या फिर मुस्लिम बहुल देश हैं। इस्लाम, अपने लगभग 200 करोड़ अनुयायियों के साथ, इस संसार का दूसरा बड़ा मजहब है। जिन देशों में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, वहां की अधिकतर सरकारों या फिर अन्य गैर-इस्लामी मतावलंबियों के साथ उनका तनाव है। भारत के साथ फ्रांस, ब्रिटेन सहित अधिकतर यूरोपीय देश, चीन और अमेरिका आदि इसके जीवंत उदाहरण हैं।
सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि जो राष्ट्र घोषित रूप से इस्लामी हैं या शरिया द्वारा संचालित हैं, वहां भी मुसलमानों का अपने अन्य मुस्लिम बंधुओं के साथ मजहब के नाम पर हिंसक टकराव है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, यमन ईरान, इराक आदि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस संकट का प्रमुख कारण— मुस्लिम समाज में व्याप्त कालबह्यी मध्यकालीन अवधारणाओं का सर्वमान्य जीवन मूल्यों से द्वंद्व है।
इस संबंध में मिस्र के प्रधान मुफ्ती डॉ. शौकी इब्राहिम अब्देल करीम अल्लाम का हालिया भारत दौरा (1-6 मई) महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉ. शौकी का ‘उम्माह’ में विशेष स्थान है, तो उनके विचार असंख्य मुस्लिमों के लिए अनुकरणीय। अपनी इस यात्रा में उन्होंने 5 मई को एक बहुसंस्करणीय अंग्रेजी समाचार पत्र में कॉलम लिखते हुए आह्वान किया था, “आधुनिक दुनिया के साथ इस्लाम को सामंजस्य बनाना, मुसलमानों के लिए आवश्यक हो गया है।”
ऐसा नहीं है कि एकेश्वरवादी अब्राह्मी मजहबों में अपनी मान्यता, पहचान और जीवनशैली को सामयिक बनाने का प्रयास पहली बार हो रहा है। बीते कुछ दशकों में वैश्विक ईसाई मतावलंबियों के वर्ग ने अपनी कई कालबह्य मजहबी अवधारणाओं को तिलांजलि दोकर, तो यहूदियों ने अपनी मान्यताओं से समझौता किए बिना स्वयं को समयानुकूल बनाया है। परंतु इस दिशा में मुस्लिम समाज को उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है।
एक सदी पहले मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने इस्लामी तुर्की को सेकुलर स्वरूप दिया था, जिसे बीते 20 वर्षों से घोर मजहबी वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन से चुनौती मिल रही है। इसी तरह ईरान को आधुनिक हेतु शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने अपने दौर (1941-1979) में अभियान छेड़ा था। परंतु इस पर आक्रोशित आयतुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी ने हिंसा के बल पर पहलवी को अपदस्थ करके वर्ष 1979-80 में ईरान को शरीयत अधीन इस्लामी गणतंत्र घोषित कर दिया। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। यक्ष प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों होता है?
डॉ. शौकी के अनुसार, “आतंकवादी हमला करने वाले मुस्लिम मानसिक रूप से ‘बीमार’ और ‘फ्रिंज माइनॉरिटी’ हैं।” क्या यह सत्य नहीं कि इस्लाम के नाम पर जिहादी हमला और अपने मजहब में सुधार का विरोध करने वाले ‘काफिर’, ‘कुफ्र’ और ‘शिर्क’ रूपी मजहबी अवधारणा से प्रेरित हैं, जो कट्टर मुसलमानों में गैर-मुस्लिमों के साथ अपने मुस्लिम बंधुओं के प्रति भी ‘सह-अस्तित्व’ की भावना को क्षीण कर देता है?
सदियों से हिंदू समाज में अस्पृश्यता व्याप्त है, जिसके परिमार्जन हेतु समाज के भीतर से आवाज उठी। ऐसे सतत आंतरिक प्रयासों का परिणाम है कि स्वतंत्र भारत में आरक्षण—व्यवस्था लागू है और बौद्धिक स्तर पर छुआछूत का कोई समर्थन नहीं करता। इसी कारण देश में सती-प्रथा कोई मुद्दा नहीं, पर्दा/घूंघट प्रथा नगण्य, कन्या-भ्रूण हत्या पर कानूनी रोक, तो समाज दहेज, बाल-विवाह आदि के प्रति कहीं अधिक जागरूक है। यह सब इसलिए भी संभव हो पाया, क्योंकि इन कुरीतियों का वैदिक वांग्मय में कोई उल्लेख नहीं है। इस पृष्ठभूमि में क्या मुस्लिम समाज में सुधार की अपेक्षा की जा सकती है?
अंतर-मजहबी संवाद के पक्षधर डॉ. शौकी ने अपने कॉलम में यह भी लिखा था, “इस्लाम और भारतीय संस्कृति, अलग-अलग मूल्य प्रणालियां हैं। इन मतभेदों का सम्मान ही सह-अस्तित्व का आधार है।” जब मुफ्ती साहब ऐसा कहते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि बहुलतावाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र— अनादिकाल से भारतीय सनातन संस्कृति का प्रतिबिंब है। इसलिए सदियों पहले जब पारसी, यहूदी, सीरियाई ईसाई आदि अपने उद्गम स्थान पर मजहबी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण लेने आए, तब उनका स्थानीय हिंदू शासकों और समाज द्वारा स्वागत किया गया, तो उन्हें उनकी पूजा-पद्धति का अनुसरण करने की सुविधा भी दी गई।
मिस्र के बहुसंख्यक मुसलमानों का अपनी पूर्व-इस्लामी सभ्यता के साथ कोई संघर्ष नहीं है। परंतु भारत में विरासत, संस्कृति और पूर्वज सांझे होने के बाद भी हिंदू-मुस्लिम में टकराव है। भारतीय मुस्लिमों का एक वर्ग न केवल अपनी मूल पहचान से घृणा करता है, अपितु बाबर, गजनवी, औरंगजेब, टीपू जैसे इस्लामी आक्रांताओं को अपना प्रेरणास्रोत मानता है, जिन्होंने ‘काफिर-कुफ्र’ अवधारणा से प्रेरित होकर भारत की सनातन संस्कृति और उसके प्रतीक-चिन्हों पर असंख्य कुठाराघात किए थे।
विश्वभर की पूजा-पद्धतियों को चाहिए कि वे अपनी कालबह्य अवधारणाओं को परिमार्जित करके उसे शाश्वत ‘सह-अस्तित्व’ की भावना से युक्त बनाएं। इस दिशा में इस्लाम को समकालीन बनाने का प्रयास तभी संभव है, जब इसके लिए मुस्लिम समाज के भीतर से निरंतर आवाज उठे।
(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार, पूर्व राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय-उपाध्यक्ष हैं)