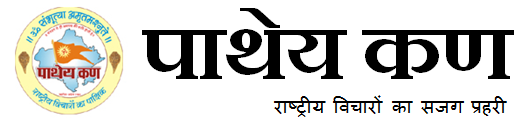38 को फांसीः स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी सजा

प्रमोद भार्गव
 38 को फांसीः स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी सजा
38 को फांसीः स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी सजा
14 साल पहले क्रमवार बम धमाकों से गुजरात के अहमदाबाद को दहला देने वाले 38 आतंकवादियों को दोषी ठहराते हुए विशेष अदालत ने फांसी की सजा दी है, जो स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी सजा है। इसी मामले में 11 अन्य दोषियों को आखिरी सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इन देशद्रोही क्रूर आतंकियों ने 26 जुलाई 2008 को समूचे अहमदाबाद को आतंक की चपेट में लेते हुए 56 लोगों की जान ले ली थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इनमें से कई स्थाई विकलांगता और मानसिक रोग का शिकार हो गए हैं। इसके पहले इतनी बड़ी मौत की सजा 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल 26 दोषियों को तमिलनाडु की टाडा अदालत ने सुनाई थी। ये आतंकी मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर-प्रदेश और कर्नाटक के रहने वाले हैं। अतएव इनका जाल लगभग पूरे देश में फैला हुआ था। इस कठोर फैसले से जहां न्याय के प्रति विश्वास पैदा होता है, वहीं इसमें 14 साल का लंबा समय लगा, इससे यह भी पता चलता है कि न्याय की गति 21वीं सदी के कम्प्यूटर युग में भी कछुआ चाल से चल रही है। अभी भी यह कहना मुश्किल है कि इन्हें जल्द फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा? इस मामले की अपील ऊपर की अदालतों में की जाएगी। यदि आतंक व देशद्रोह से जुड़ा मामला होने के कारण निपटारा जल्द भी होता है तो राष्ट्रपति के यहां लगाई जाने वाली दया याचिकाएं, इनके जिंदा रहने की मियाद बढ़ाए रखेंगी। हालांकि कुछ समय से धन लेकर मानवाधिकारों के हनन की वकालत करने वाले कथित समाजसेवियों की संख्या में कमी आई है। फिर भी मृत्युदंड को टालने के प्रावधानों पर वैधानिक अंकुश लगाने की आवश्यकता है।
भारत में मृत्युदंड लगातार बहस का मुद्दा बना रहा है। परंतु शीर्ष न्यायालय का फैसला जो भी हो, भारतीय दंड संहिता में जब तक मौत की सजा का प्रावधान है, तब तक जघन्य अपराधों में अदालत मौत की सजा देती रहेगी। इस सजा को समाप्त करने का अधिकार संसद को है। और संसद एकमत से हत्या की धारा 302 और देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की धारा 121 को विलोपित करने का विधेयक पारित करा ले, ऐसा निकट भविष्य में संभव भी नहीं है। संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरू और मुंबई हमले के एकमात्र जिंदा बचे पाकिस्तानी हमलावर अजमल आमिर कसाब आदि को मृत्युदंड के बाद फांसी के फंदे पर लटकाया भी गया है। ये दोनों ही मामले दुर्लभतम होने के साथ देश की संप्रुभता को चुनौती देने की राष्ट्र विरोधी मुहिम से जुड़े थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खालिस्तान सर्मथक आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर का अपराध भी अफजल और कसाब की प्रकृति का है, इसलिए भुल्लर के अपराध को इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए? हालाँकि भुल्लर मामले में 12 अप्रैल 2013 को अदालत ने कहा भी था कि दया याचिका पर फैसले में देरी फांसी की सजा माफ करने का आधार नहीं बन सकती है। इसी तरह बाटला हाउस में शामिल रहे आजमगढ़ के हत्यारे आतंकियों और लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी इसरत जहां को निर्दोष बताने की देशव्यापी मुहिम कथित सामाजिक कार्यकर्ता व कुछ प्रमुख नेताओं ने छेड़ी हुई थी। ऐसे देशद्रोही अपराधियों के पक्ष में जनमत बनाने का अभियान विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठन शामिल रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की आतंक पर लगाम लगाने की दृढ़ता के चलते इन एनजीओ की अब आवाजों पर ताले पड़े हुए हैं।
दरअसल देशद्रोह और जघन्य से जघन्यतम अपराधों में त्वरित न्याय की आवश्यकता तो है ही, दया याचिका पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की जरूरत भी है। शीर्ष न्यायालय ने यह तो कहा है कि दया याचिका पर तुरंत फैसला हो, लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्या समय सीमा होनी चाहिए, यह सुनिश्चित नहीं है। क्योंकि अक्सर राष्ट्रपति दया याचिकाओं पर निर्णय को या तो टालते हैं या फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलते हैं। हालांकि महामहिम प्रणब मुखर्जी इस दृष्टि से अपवाद रहे हैं। उन्होंने ही अफजल गुरू और अजमल कसाब की दया याचिकाएं खारिज कर उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाने का रास्ता साफ किया था। जबकि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने या तो दया याचिकाएं टालीं या मौत की सजा को उम्र कैद में बदला। यहां तक कि उन्होंने महिला होने के बावजूद बलात्कार जैसे अपराध में फांसी पाए पांच आरोपियों की सजा आजीवन कारावास में बदली थी।
दरअसल दया याचिका के चलते विलंब होता है तो मौत की प्रतीक्षा कर रहे कैदी मानसिक रोगी हो सकते हैं? इस आधार पर मानसिक रूप से विक्षिप्त कैदी को फांसी की सजा देना उचित नहीं माना जाता। वास्तव में दया याचिकाओं पर अंतिम निर्णय में होने वाली देरी के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल ज़िम्मेदार होते हैं। लेकिन ये दोनों ही पद संवैधानिक हैं, इसलिए अदालतें इन पर टिप्पणी करने में संवैधानिक मर्यादा का पालन करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों को दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार मिला हुआ है। चूंकि ये देश और राज्यों के सर्वोच्च पद हैं, इसलिए संविधान निर्माताओं ने दया याचिका पर निर्णय को समय की सीमा में नहीं बांधा। हालांकि दया-याचिका पर कानूनी प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था की बाध्यता के चलते महज कागजी खानापूर्ति भर है, लिहाजा इन सर्वोच्च पदाधिकारियों को भी अपनी जवाबदेही महसूस करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में दया-याचिकाओं पर अनावश्यक विलंब न हो।
हालांकि किसी भी देश के उदारवादी लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था आंख के बदले आंख या हाथ के बदले हाथ जैसी प्रतिशोधात्मक मानसिकता से नहीं चलाई जा सकती? लेकिन जिन देशों में मृत्युदंड का प्रावधान है, वहां यह मुद्दा हमेशा ही विवादित रहता है कि आखिर मृत्युदंड सुनने का तार्किक आधार क्या हो? इसीलिए भारतीय न्याय व्यवस्था में लचीला रुख अपनाते हुए गंभीर अपराधों में उम्र कैद एक नियम और मृत्युदंड अपवाद है। इसीलिए देश की शीर्षस्थ अदालतें इस सिद्धांत को महत्व देती हैं, कि अपराध की स्थिति किस मानसिक परिस्थिति में उत्पन्न हुई? अपराधी की सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों व मजबूरियों का भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि एक सामान्य नागरिक सामाजिक संबंधों की जिम्मेदारियों से भी जुड़ा होता है। ऐसे में जब वह अपनी बहन, बेटी या पत्नी को बलात्कार जैसे दुष्कर्म का शिकार होते देखता है तो आवेश में आकर हत्या तक कर डालता है। भूख, गरीबी और कर्ज की असहाय पीड़ा भोग रहे व्यक्ति भी अपने परिजनों को इस जलालत की जिदंगी से मुक्ति का उपाय हत्या में तलाशने को विवश हो जाते हैं। स्पष्ट है, ऐसे मजबूरों को मौत की सजा के बजाय सुधार और पुनर्वास के अवसर मिलने चाहिए? क्योंकि जटिल होते जा रहे समय में दंड के प्रावधानों को तात्कालिक परिस्थिति और दोषी की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी आंकना जरूरी है। परंतु बलात्कार और फिर महिला की हत्या भिन्न प्रकृति के अपराध हैं।
दया याचिका पर सुनवाई के लिए यह मांग हमारे यहां उठ रही है कि इसकी सुनवाई का अधिकार अकेले राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में न हो? इस हेतु एक बहुसदस्यीय जूरी का गठन हो। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, उप राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और कुछ अन्य विषेषाधिकार संपन्न लोग भी शामिल हों? यदि इस जूरी में भी सहमति न बने तो इसे दोबारा शीर्ष अदालत के पास प्रेसिडेंशियल रेंफरेंस के लिए भेज देना चाहिए। इससे गलती की गुंजाइश न्यूनतम हो सकती है? इसके उलट एक विचार यह भी है कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का प्रावधान समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही अंतिम फैसला माना जाए? यह विचार अधिक तार्किक है, क्योंकि न्यायालय अपराध की प्रकृति, अपराधी की प्रवृति और परिस्थिति के विश्लेषण के तर्कों से सीधे रूबरू होती है। फरियादी का पक्ष भी अदालत के समक्ष रखा जाता है। जबकि राष्ट्रपति के पास दया याचिका पर विचार का एकांगी पहलू होता है? स्पष्ट है न्यायालय के पास अपराध और उससे जुड़े दंड को देखने के कहीं ज्यादा साक्ष्यजन्य पहलू होते हैं। परिणामस्वरूप तर्कसंगत उदारता अदालत ठीक से बरत सकती है।
(लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं)