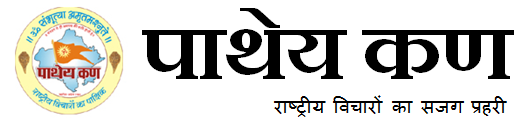बाबा और समाज

बलवीर पुंज
 बाबा और समाज
बाबा और समाज
उत्तरप्रदेश के हाथरस में गत दिनों एक सत्संग में भगदड़ मचने से 123 भक्तों की कुचलकर मौत हो गई। अधिकांश मृतक अनुसूचित जाति समाज के थे। साधारणत: किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति उत्पीड़न-हत्या-दुर्घटना का मामला, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बन जाता है। परंतु हाथरस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अव्यवस्था-लापरवाही बरतने का आरोप भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव पर है, जोकि स्वयं भी अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। चूंकि यह घटना ‘दलित बनाम सवर्ण’ या ‘जातिगत तनाव’ नैरेटिव के अनुकूल नहीं है, इसलिए इस पर मौन की दहाड़ है। खैर, इस कॉलम का विषय यह नहीं है।
हाथरस मामले ने इस प्रकार के ‘गॉडमैन’ बाबाओं को पुन: चर्चा में ला दिया है। आखिर नारायण साकार हरि के साथ गुरमीत सिंह, राधे-मां, आशुतोष महाराज, निर्मल बाबा, रामपाल, आसाराम बापू जैसे कथित बाबाओं से लाखों-करोड़ की संख्या में लोग क्यों जुड़ जाते हैं? इनकी जीवन-शैली, वेशभूषा और आचार-व्यवहार भारत के पारंपरिक संतों के बिल्कुल विपरीत है और उनके उद्बोधनों में कोई पांडित्य भी प्रकट नहीं होता है। क्या कारण है कि इन तथाकथित ‘बाबाओं’ के लिए उनके अनुयायी मरने-मारने को भी तैयार रहते हैं? कई राजनीतिक दल भी उनके अनैतिक और गैर-कानूनी कार्यों में या तो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग देते हैं या फिर उन पर चुप्पी साधे रखते हैं।
यह उपक्रम न तो हिंदू समाज तक सीमित है और न ही अकेले भारत इसका शिकार है। पंजाब सहित देश के कई क्षेत्रों में आयोजित चंगाई सभाओं में पादरी अंधे-अपंग और रोगी व्यक्ति को अपने ‘करिश्मे’ से ठीक करने का दावा करते हैं। इनमें अवैध-अनैतिक रिलीजियस कन्वर्जन किसी से छिपा नहीं है। ईसाई बहुल अमेरिका-ब्रिटेन आदि विकसित देशों के साथ इस्लामी दुनिया में भी पीर-फकीर का तिलिस्म फैला हुआ है, जिससे वहां का सत्ता-अधिष्ठान भी प्रभावित है। पाकिस्तान में पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी तीसरी बेगम पीर बुशरा मेनका की ‘रुहानी ताकत’ की खूब चर्चा रही है।
भारत में बाबाओं की सफलता का एक बड़ा कारण शासकीय विफलता है। कोई भी व्यवस्था जितनी अक्षम और भ्रष्ट होगी, समाज में उतनी ही अनिश्चितता और असंतोष बढ़ेगा। यह स्थिति सूरजपाल आदि बाबाओं के लिए सबसे अनुकूल है। देश-प्रदेश में सरकार भले ही किसी की हो, उसके अधीनस्थ तंत्र अक्सर संवेदनहीन होता है। देश का बहुत बड़ा हिस्सा दशकों से अपनी आवश्यकताओं (राशन-चिकित्सा-शिक्षा सहित) की पूर्ति के लिए सरकारी उपक्रमों पर निर्भर है। परंतु जन-सरोकार हेतु स्थापित सार्वजनिक निगम-विभाग (पुलिस थाना सहित), बैंक, अस्पताल, स्कूल इत्यादि घूसखोरी, धांधली और उत्पीड़न के पर्याय बन चुके है। यहां जनता स्वयं को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करती है। बीते कुछ वर्षों से इस स्थिति में ‘डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर’ प्रक्रिया से बदलाव आया है, जिसमें लाभार्थियों को तहसीलदारों के चक्कर लगाए बिना सीधा सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। परंतु शेष व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर आज भी सड़ी-गली है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है।
वर्षों पुरानी शासकीय प्रणाली और उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था की अक्षमता-असफलता का लाभ स्वयंभू ‘चमत्कारी’ बाबाओं को मिलता है। देशभर में इनके कई सौ एकड़ में फैले शिविरों में निशुल्क या सस्ती सुविधायुक्त चिकित्सा प्रणाली, दवा केंद्र, शिक्षा, खेल-उद्यान आदि उपलब्ध हैं, जिन्हें पाकर उनके करोड़ों अनुयायी स्वयं को सम्मानित अनुभव करते हैं। यह हजारों-लाखों लोगों को स्वयंभू बाबाओं से जोड़ने में बड़ा कारक है।
आधुनिकता और निजी स्वतंत्रता के नाम पर शासकीय व्यवस्था नशा-धूम्रपान और लिव-इन संबंधों (समलैंगिकता सहित) को सशर्त स्वीकृति देती है। परंतु समाज का बड़ा वर्ग इन्हें स्वीकार नहीं कर पाता है। जहां शराब सेवन से लाखों परिवार बर्बाद हो गए है, तो लिव-इन संबंधों को समाज में अब भी व्यभिचार-अनैतिक माना जाता है। भले ही बाबाओं का निजी जीवन कैसा भी हो, परंतु इन विषयों पर वे व्यापक जनभावना को साझा करते हैं।परिणामस्वरूप, उनकी लोकप्रियता बनी रहती है।
मानवीय जीवन अनिश्चिताओं से भरा है और बहुत से मामलों में मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता। उपभोक्तवादी दौर में अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य से ऊपर धन-पद अर्जित करने और सुख-सुविधा पाने की लालसा बढ़ गई है। इसमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर कई लोग इन्हीं बाबाओं के शरण में चले जाते हैं, जो भले ही उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हों, परंतु अपने आभामंडल से उन्हें कुछ मानसिक संतुष्टि अवश्य प्रदान करते हैं। यही नहीं, बढ़ते शहरीकरण के कारण वे बिरादरियां और अन्य सामाजिक संरचनाएं तेजी से टूट रही हैं, जो कुछ दशक पहले तक व्यक्ति को पहचान और सुरक्षा का भाव देती थीं। वर्तमान सामाजिक ताने-बाने में उस भावनात्मक सुरक्षा का अभाव है, जिसकी पूर्ति करने में स्वयंभू बाबा और उनकी मंडली बड़ी भूमिका निभाते हैं।
आधुनिक शासकीय व्यवस्था अक्सर मानवीय आवश्यकताओं- रोटी, कपड़ा और मकान से बाहर नहीं जाता। ठीक है कि प्रत्येक मानव की यह मूल आवश्यकता है। परंतु उनकी एक और आवश्यकता भी होती है, जिसे हम अध्यात्म, भावनात्मक या फिर ‘अपनेपन की भावना’ के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसके प्रति राजकीय उदासीनता भी लोगों को स्वयंभू ‘साधु-संतों’ से जोड़ रही है। भारतीय जीवन-पद्धति और उसकी शैली के केंद्र में आध्यात्मिकता है, जो किसी मजहबी दर्शन जैसी संकीर्ण नहीं है। वैदिक सनातन संस्कृति प्रदत्त इस चेतना को गत कई सदियों से अनेकों महानुभावों (सिख परंपरा, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, गांधीजी, विनोबा भावे सहित) ने आगे बढ़ाया है। परंतु छद्म-सेकुलरवाद के नाम पर स्वतंत्र भारत में जिस तरह की विकृत व्यवस्था स्थापित की गई है, उसमें सत्ता-अधिष्ठान द्वारा आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना— ‘सांप्रदायिक’ चश्मे से देखा जाने लगा है। शासन-व्यवस्था और समाज के बीच आए इस खालीपन को स्वघोषित ‘संत’ या ‘गुरु’ अपने निजी लाभ हेतु बड़ी चतुराई, छल-फरेब और आधुनिक विशेष प्रभावों के साथ भर देते हैं।
श्रीमद्भगवद्गीता में कर्म की प्रधानता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि हम इसे अपने जीवन का सार बना लें, तो समाज में ‘गॉडमैन’ बाबाओं की उपयोगिता क्षीण होकर एक दिन समाप्त हो जाएगी। क्या ऐसा निकट भविष्य में संभव है?
(हाल ही में लेखक की ‘ट्रिस्ट विद अयोध्या: डिकॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया’ पुस्तक प्रकाशित हुई है)