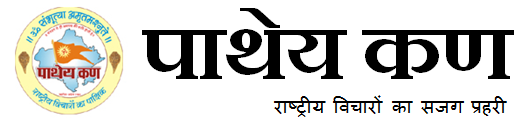मेरी हिन्दी

डॉ. अरुण सिंह
 मेरी हिन्दी
मेरी हिन्दी
अंग्रेज़ी के अतिरिक्त या इस से अधिक हिन्दी का प्रयोग मेरे लिए किसी पूर्वाग्रह अथवा महत्वाकांक्षा का विषय नहीं रहा। हिन्दी तो छुटपन में ही चेतना में बस गई। सरलता और सहजता से।
बचपन मारवाड़ के रेगिस्तानी अंचल में बीता। घर में ब्रज, बाहर मारवाड़ी और स्कूल में अध्ययन के दौरान हिन्दी। ये सब अलग नहीं थे। कड़ी एक ही थी। वह थी, मूल सांस्कृतिक चेतना। इसी में धर्म और भाषा अटूट रूप से निहित हैं। यह वही है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सनातन काल से सहेजा है और अभी तक अस्तित्व में है। भाषाएं बदली हैं, पर हमारी सांस्कृतिक चेतना नहीं। आक्रमणकारी संस्कृतियों को भी हमारी भाषाओं ने आत्मसात किया, पर यह दुःखद है कि आज निरपेक्षतावादी दावों के प्रभाव में हमारी मूल चेतना को हाशिए पर रखा जाता है अथवा विभाजनकारी विमर्शों के माध्यम से छिन्न भिन्न करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है।
रात्रिकाल में मारवाड़ी में विक्रम वेताल की कहानियों का श्रवण, स्कूल के पाठ्यक्रम में साहित्य की चुनिंदा कविताएं और कहानियां, देसी खेल, धोरे की रेत पर लुढ़कना, फुटबॉल, खो खो, पशु-पक्षी, सिरस की सुवास — सब में शाश्वत, विशुद्ध हिन्दी थी, मूल भारतीय चेतना का परम आनन्द।
मेरी प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाई नब्बे के दशक में हुई। स्कूल के अध्यापक उन दिनों आज से बहुत अलग हुआ करते थे। भौतिकवाद इतना नहीं था। अध्यापकों का घर तक संपर्क हुआ करता था। मातृ पितृ तुल्य स्नेह से सिंचित थे हम उन दिनों स्कूल में भी। सार की बात यह है कि अंग्रेज़ी का अस्तित्व था, पर अंग्रेजियत नहीं थी। हिन्दी हमें देशीयता में सींचती थी। आज की अदृश्य रूप से घुलती हुई, घेरती हुई, निगलती हुई मिशनरी संस्कृति हमसे दूर थी।
मेरे लिए आज भी हिन्दी वही है। यह मुझे वहीं ले जाती है, मेरी मूल सांस्कृतिक और साभ्यतिक चेतना में, जो मेरे अस्तित्व में निहित है। यह मुझे अंग्रेज़ी पढ़ने लिखने से मना नहीं करती, बस अंग्रेजियत के प्रभाव तले दब न जाने का आग्रह मात्र करती है। क्योंकि महर्षि श्री अरविंद के शब्दों में हम स्वयं पर नियंत्रण करने वाली संस्कृति हैं, स्वराट हैं हम।