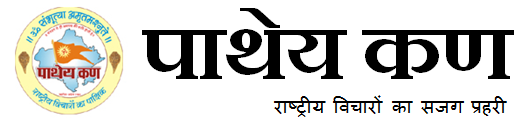राष्ट्र-संस्कृति से आप्लावित पं. दीनदयाल उपाध्याय का राजनैतिक दर्शन

कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल
 राष्ट्र-संस्कृति से आप्लावित पं. दीनदयाल उपाध्याय का राजनैतिक दर्शन
राष्ट्र-संस्कृति से आप्लावित पं. दीनदयाल उपाध्याय का राजनैतिक दर्शन
भारतीय राजनीति के वृहद आकाश में दैदीप्यमान पं. दीनदयाल उपाध्याय अपने राष्ट्रीय विचारों, राष्ट्र प्रेम व भारतीय सनातन हिन्दू संस्कृति के मुखर पक्षधर व तदानुरुप रीति-नीति के आधुनिक राजनैतिक प्रवर्तकों में लब्ध-प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने केवल विचार ही नहीं दिए, अपितु जनसंघ व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से विचारों को धरातलीय रूप भी दिया। एकात्म मानव दर्शन और अन्त्योदय जैसे मूल्य जनसंघ से होते हुए वर्तमान भाजपा की नीतियों में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। पण्डित जी विचारकों में प्रतिष्ठित व सुशोभित होने के साथ-साथ ही अपने चिन्तन व दर्शन के बहुआयामी व लोकल्याणकारक मान-बिन्दुओं के द्वारा जहाँ नूतन प्रस्थापनाएँ करते हैं। वहीं वैचारिक एवं कार्य स्तर पर कई सारी भ्रामक, अहितकारी रूढ़ियों को तोड़ते हुए भारतीयता के अनुरूप मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके विचार एवं दर्शन के विविध रुप हैं जिनमें उनका राजनैतिक दर्शन भी अपने आप में अनूठा है। उनके राजनैतिक दर्शन के मूल में भी – ‘राष्ट्र’, संस्कृति, धर्म, उच्च आदर्श और समाज है। वे स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं कि ‘राजनीति राष्ट्र के लिए’ ही होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की संकीर्णता या स्वार्थ प्रेरित हित लाभ के दृष्टिकोण- अराष्ट्रीय प्रवृत्ति एवं भारत की राष्ट्रीयता के लिए एक प्रकार का खतरा ही हैं। वे राजनैतिक शुचिता व राजनीति, दल, विचारधारा के मूल में राष्ट्रोन्नति व जनकल्याण को ही रखते हैं तथा येनकेन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति तथा अवसरवादिता व मूल्यों से पृथक राजनीति को तिलाञ्जलि देते हैं।
पण्डित जी भारतीय राजनीति व वैश्विक राजनीति में अपना प्रभाव रखने वाली विचारधाराओं की तात्विक समीक्षा करते हुए उनका नीर-क्षीर विवेचन करते हैं। साथ ही स्वातन्त्र्योत्तर काल के उपरान्त पश्चिमी प्रभाव से ग्रस्त राजनीतिज्ञों की ‘स्वदेशी’ की ओर न देखकर पश्चिम का अन्धानुकरण करने का विरोध करते हैं और इन प्रवृत्तियों को भारत व भारतीयता के लिए आत्मध्वन्सात्मक बतलाते हैं। उनके मतानुसार – आधुनिक पाश्चात्य देशों का उदय केवल पाँच सौ से सात सौ वर्षों की अवधि के पूर्व ही हुआ है, किन्तु भारत हजारों वर्षों से आसेतु हिमालय की भाँति एक उत्कृष्ट राष्ट्र के रूप में अवस्थित है। अतएव वे पाश्चात्य देशों की कसौटी और उनके निष्कर्षों पर भारत के आँकलन व अनुकरण करने को न्यायसंगत नहीं मानते हैं। दीनदयाल जी का मानना था कि – “जो हमारा है उसे समयानुकूल बनाया जाए तथा जो विदेशी है, उसे राष्ट्रानुकूल बनाया जाए। भारतीय समाज में केवल विदेशी होने के कारण श्रेष्ठताबोध और भारतीय होने के कारण उसे उपेक्षित और नकारने की दुष्प्रवृत्ति का विरोध करते हैं।”
चूँकि पराजयबोध व हीनभावना की व्याप्ति अकादमिक स्तर पर तथा राजनैतिक अन्धानुकरण के कारण क्रमशः स्थापित की गई। इसलिए वे इस पर तीक्ष्ण प्रहार करते हुए कहते हैं :― स्वत्व एवं स्वाभिमान का मेरुदण्ड सीधा तना न हो तो विश्व में भौतिक दृष्टि से बलशाली, प्रभावशाली,विजयशाली तथा वैभवशाली माने जाने वाले राष्ट्रों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति बल पकड़ती है। अपने पिछड़े और दरिद्र समाज से लज्जा आने लगती है। यह अनुसरण बड़ी बातों से लेकर छोटी-छोटी दैनिक बातों तक छनता चला आता है।
विभिन्न विचारधाराओं व पश्चिमी व्यवस्थाओं को लेकर उनका गहन अध्ययन रहा है। वे व्यापक शोध एवं विश्लेषण के उपरान्त निष्कर्षत: यह कहते हैं कि -पश्चिम की नकल ‘मॉडर्न’ होने का प्रमाण बन गया है,यह चहुँमुखी अनुकरण ठीक नहीं, क्योंकि पश्चिमी चिन्तन और व्यवस्था मानव कल्याण में असफल रही है। आगे वे मैकॉले शिक्षा प्रणाली और उसके दुष्प्रभाव पर कहते हैं – किसी ने स्वदेशी पर जोर दिया तो उसे असभ्य बता दिया जाता है। हम ब्रिटिशों से हार गए। चालाक मिशनरियों तथा शासकों ने मैकॉले शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हमारे मन में अनेक बीज बो दिए। तब से हमारे शिक्षितों में और उनकी देखादेखी समाज के अन्य लोगों में भी पाश्चात्यों के अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई है। स्वतन्त्रता के बाद तो वह निरंकुश हो गई है।
जहाँ वे मार्क्स के दर्शन के पूर्णतः ‘भौतिकवादी’ होने के सिद्धांत को अनुपयुक्त मानते हैं, जिसके उदाहरण रूस, चीन इत्यादि भरे पड़े हैं। वहीं ‘समाजवाद’ और ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ के द्वारा मनुष्य की स्वतन्त्रता की समाप्ति व उसके द्वारा मानवीय जीवन में राज्य के वर्चस्व को भी अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि लोकतान्त्रिक समाजवाद जैसी कोई चीज नहीं है, शब्द भर है। क्योंकि समाजवाद लाने में लोकतन्त्र की हत्या करनी पड़ती है। साथ ही उन्होंने पूँजीवादी व्यवस्था को भी मानव कल्याण के लिए असफल माना है। इन सबका हल सुझाते हुए वे कहते हैं :― विश्व की समस्याओं का हल समाजवाद पूँजीवादी लोकतन्त्र नहीं, वरन् हिन्दूवाद है। यही एक ऐसा जीवनदर्शन है जो जीवन का विचार करते समय उसे टुकड़ों में नहीं बाँटता, अपितु सम्पूर्ण जीवन को इकाई मानकर उसका विचार करता है। वे इसे हिन्दूवाद, मानवतावाद या चाहे जिस रूप में स्वीकार किए जाने की बात करते हुए स्पष्ट करते हैं कि -यही भारत की आत्मा के अनुरूप व जनमानस में उत्साह को सञ्चारित करेगा, साथ ही विभ्रान्ति के चौराहे में खड़े विश्व के लिए मार्गदर्शक के रूप में भी काम करेगा।
वे राष्ट्र को जीवमान इकाई मानते हुए कहते हैं कि – एक भूमि विशेष में रहने वाले लोगों का, जिनके ह्रदय में मातृभूमि के प्रति असंदिग्ध श्रद्धा का भाव हो, जिनके जीवनादर्शों में साम्य हो, जीवन के प्रति स्पष्ट दृष्टि हो, शत्रु-मित्र समान हों, ऐतिहासिक महापुरुष एक हों; इन सबसे राष्ट्र का निर्माण होता है। इसके विपरीत आक्रान्ता से इसलिए सहानुभूति रखना कि वे हम-मजहब हैं, अराष्ट्रीय प्रवृत्ति है। वैश्विक राजनीति व भारतीय परिदृश्य में ‘राष्ट्रवाद’ सर्वदा चर्चित रहता है, भारत की वामपंथी विचारसरणी, सिद्धांत विहीन दल- भारतीय राष्ट्रवाद को प्रायः हिटलर, मुसोलिनी से जोड़कर लाँछित करने लगते हैं। जबकि यह सर्वज्ञात तथ्य है कि भारतीय राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही स्वातन्त्र्य यज्ञ सफल हुआ था, अन्यथा स्वतन्त्रता असंभव सी थी।
पण्डित जी राष्ट्रवाद के सन्दर्भ में विस्तृत व्याख्या करते हुए कहते हैं – यूरोपीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्र प्रेम में अन्तर है। यूरोपीय चिन्तन पारस्परिक संघर्ष की अवधारणा पर आधारित है। जबकि भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म संघर्ष में नहीं हुआ है,अपितु सभ्यता के आरम्भ से ही भारत सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है ; जिसमें कई राजनैतिक सत्ताएँ थी किन्तु ‘राष्ट्र’ एक था। भारत का राष्ट्रीय विचार न तो विस्तारवादी है, न ही साम्राज्यवादी और आक्रमणशील बल्कि भारतीय विचार ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ पर आधारित है जो प्राणिमात्र के प्रति कल्याण का भाव रखता है। भारतीय विचार की तुलना पर वे कहते हैं – पश्चिम के राष्ट्रवाद से भारत के विचार की तुलना करना ही गलत है। पश्चिम ने द्वैत के आधार पर संघर्ष का नगाड़ा बजाया और भारत ने अद्वैत के आधार पर एकात्म की बाँसुरी बजायी। दोनों वाद्य होते हुए भी दोनों की स्वरलहरियों में भारी अन्तर है। इस भेद को समझकर हमें राष्ट्रीयता का विचार करना चाहिए।
वे भूमि, जन, संस्कृति के संघात से राष्ट्र के निर्माण की बात कहते हैं।और संस्कृति का अभिप्राय ही ‘हिन्दू संस्कृति’ है तथा उनके मतानुसार भारतीय राष्ट्रीयता का आधार यह संस्कृति है। भारत की एकात्मकता तभी सम्भव है, जब संस्कृति के प्रति निष्ठा रहे। वे हिन्दू संस्कृति शक्ति व सांस्कृतिक राष्ट्रप्रेम के सम्बन्ध में यथार्थबोध प्रस्तुत करते हैं – भारतीय राष्ट्रीयता सांस्कृतिक राष्ट्रप्रेम है, क्योंकि भारतवर्ष को राजनीति और हमलावरों ने कई बार विखण्डित किया, किन्तु संस्कृति ने उसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखण्ड रखा। जहाँ हिन्दू संस्कृति और हिन्दू धर्म कमजोर हुआ वह हिस्सा भी देश से कट गया। इन्हीं सब कारणों के चलते भारत और भारतीयता की मूल पहचान के रूप में हिन्दू संस्कृति को केन्द्र व मानबिन्दु के रूप में रखते हैं। साथ ही वे भारत में व्याप्त विविधताओं में पृथकता के स्थान पर ‘एकत्व’ को प्रतिष्ठित करते हुए भाषा,प्रान्त, वेशभूषा,खान-पान,रहन-सहन उपासना पध्दति के आधार पर किसी भी प्रकार के विभाजन की विकृति को अस्वीकार करते हैं। और सभी के मध्य सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोई हुई माला के रुप में राष्ट्रीय चेतना व भारतमाता की भव्य झाँकी को देखते हैं।
वे विवेकानन्द की परम्परा का पथानुसरण करते हुए कहते हैं – हमारा धर्म (नॉट रिलिजन) हमारे राष्ट्र की आत्मा है। बिना धर्म के राष्ट्र जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता है। भारत धर्म प्राण देश है, और राष्ट्र का जातीय उद्देश्य ‘धर्म’ है, क्योंकि भारत में धर्म पर अभी आघात नहीं हुआ। अतः यह जाति जीवित है। वे अल्पसंख्यक अवधारणा को ‘प्रच्छन्न द्विराष्ट्रवाद’ या बहुराष्ट्रवाद मानते हैं। भारतीय मुसलमानों के इस्लामिक परावलम्बन, राजनैतिक हठधर्मिता, राष्ट्र-संस्कृति के प्रति अलगाव के कारण भारत में व्याप्त मुस्लिम समस्या का समाधान सुझाते हुए -मुस्लिमों के राजनैतिक पराभव व राष्ट्रवादियों द्वारा उनके समावेश का मार्ग बतलाते हैं।
पन्थनिरपेक्षता के सम्बन्ध में भी दीनदयाल जी स्पष्ट हैं, वे इस पाश्चात्य अवधारणा के सम्बन्ध में कहते हैं-सेक्युलरिज्म भारतीय धरती पर बलात् रोपा गया विदेशी पौधा है। इसके सही स्वरूप को न समझ पाने के कारण ही भारतीय राजनीतिज्ञों ने इसका अर्थ ही बदल डाला। भारत में सेक्युलरिज्म का अर्थ ‘सर्वधर्म समभाव’ के स्थान पर हिन्दू धर्म, सभ्यता, संस्कृति से जुड़ी हर बात का विरोध तथा मुसलमानों व ईसाइयों की हर उचित-अनुचित माँग का चाहे वह राष्ट्र विघातक व संविधान विरोधी क्यों न हो। इसका समर्थन करना तुष्टीकरण ही रह गया है। उनके मत में संविधान को ‘संघात्मक’ के स्थान पर ‘एकात्मक’ होना चाहिए। लोकतन्त्र में उनकी दृढ़ आस्था थी – वे व्यक्ति से अधिक दल को, दल से अधिक सिद्धांत को, सिद्धांत से ज्यादा लोकतन्त्र को और लोकतन्त्र तथा राष्ट्र में विरोध होने पर राष्ट्र को महत्व देते हैं। पण्डित जी के राजनैतिक दर्शन में भारतीयता और संस्कृति स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होती है। उनकी राष्ट्रोन्नति से आप्लावित वैचारिक चेतना में राष्ट्र के सर्वाङ्गीण विकास का दिशाबोध और स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त होता है। जो सतत् नूतन भारत को गढ़ने का मार्ग दिखाता है।