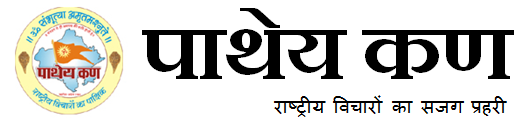जीवों के संरक्षण पर सैलेक्टिव नैरेटिव क्यों?

प्रणय कुमार
कितना अजीबोगरीब विरोधाभास है कि एक ओर तथाकथित उदारवादी बुद्धिजीवी और पेटा जैसे संगठन मानवाधिकारों, असहिष्णुता और जीवों के संरक्षण आदि की दुहाई देते हैं लेकिन दूसरी ओर बक़रीद जैसे पर्व पर लाखों निर्दोष पशुओं के सामूहिक वध की सदियों पुरानी प्रथाओं पर जड़वत मौन साध लेते हैं।
भारतीय संस्कृति में ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ एवं ‘यत पिंडे तत ब्रह्मांडे’ का महावाक्य प्रतिष्ठित रहा है। इस संस्कृति ने केवल वाणी से ही नहीं, अपितु अपने आचरण से भी यह प्रमाणित किया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही परम ब्रह्म परमात्मा की चेतना व्याप्त है। ‘जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है’ की धारणा हमें जीव-मात्र में ईश्वर-तत्व को देखने की जीवन-दृष्टि प्रदान करती है।
यह अकारण नहीं है कि हम धरती-आकाश, भूमि-पर्वत, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी से लेकर संपूर्ण दृश्य-अदृश्य नाम रूपात्मक जगत को जीवित सत्ता मानकर उसकी पूजा-अर्चना करते आए हैं। यह प्रकृति और चराचर के प्रति हमारे कृतज्ञता-भाव की अभिव्यक्ति है। छोटे-से-छोटे जीव-जंतुओं की चिंता हमारी दैनिक जीवनचर्या में सम्मिलित रही है। हमारी सहज संवेदना का विस्तार पशु-पक्षियों से लेकर वनस्पतियों-पादपों तक है। यह संवेदना का विस्तार ही मानव-जीवन का अंतिम उद्देश्य है। सभ्यता के विकास के तमाम भौतिक दावों और चरणों के मध्य भी हम इस संवेदना-तत्व को ही सर्वाधिक महत्त्व देते आए हैं। इसी के आधार पर हम किसी व्यक्ति या समूह का आकलन करते आए हैं। जीव-मात्र के प्रति इसी संवेदना के कारण क्रौंच-युगल में से एक के बिद्ध होने पर शोकार्त्त वाल्मीकि के मुख से श्लोक के रूप में करुणा की धारा फूट पड़ी थी। हमारी कला, साहित्य, संस्कृति सबके मूल में यह करुणा और संवेदना ही है।
यह सत्य है कि सनातन संस्कृति में भी काल-विशेष में युगीन परिस्थितियों से निःसृत रूढ़ियाँ प्रचलित हुईं। परंतु उन रूढ़ियों के अन्तःप्रक्षालन की एक सहज-स्वाभाविक अंतर्धारा सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। रूढ़ियों के शव को चिपकाए रखने की मनोवृत्ति सनातन समाज पर कभी हावी न होने पाई। परंपराओं और रूढ़ियों के अंतर को सनातन समाज ने बख़ूबी समझा है। अन्यथा रूढ़ियों व अंधविश्वासों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने वाले तमाम मनीषियों को सिर-माथे बिठा वह कभी उनकी गणना महापुरुषों की श्रेणी में नहीं करता।
यह भी सत्य है कि बलि-प्रथा एवं मांस-भक्षण की प्रवृत्ति सनातनियों में भी देखने को मिलती है। परंतु उसका महिमामंडन करने वाले लोग सनातनियों में गिनती के मिलेंगे।बलि-प्रथा की पैरवी तो दूर, निजता की ओट लेकर यहाँ मांस-भक्षण के सार्वजनिक पैरोकार भी गिनती के मिलेंगे। अपितु मांस-भक्षण को लेकर उनमें एक प्रकार की नैतिक फांस या ग्लानि-भावना सदैव बनी रहती है। विकल्प उपलब्ध होने पर उन्हें मांस-भक्षण को लेकर परिचितों-परिजनों तक की उपेक्षा और भर्त्सना झेलनी पड़ती है। अधिकांश की अंतरात्मा उन्हें सामिष से निरामिष की ओर जाने की स्वाभाविक प्रेरणा देती है। यहाँ की मिट्टी में ही जीव-मात्र के प्रति एक दया-भाव है।बल्कि दया-भाव से आगे सहयोग एवं सहजीविता का भाव है।सह-अस्तित्व का यह दर्शन ही सनातन को वैश्विक स्वीकृति दिलाता है। यह इसे चिर नूतन, चिर शाश्वत बनाता है।
कितनी विचित्र विडंबना और अजीबोगरीब विरोधाभास है कि एक ओर तमाम कथित उदारवादी एवं प्रगतिशील बुद्धिजीवी मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बढ़ती असहिष्णुता, वन्य-जीव संरक्षण आदि की बारंबार दुहाई देते हैं और दूसरी ओर बक़रीद जैसे पर्व पर लाखों मौन-मूक, निरीह-निर्दोष पशुओं के सामूहिक वध की सदियों पुरानी प्रथाओं पर जड़वत मौन साध लेते हैं। एक ओर उन्हें बहुसंख्यकों के आस्थाजनित आचरण में भी रूढ़ियों और अंधविश्वासों की प्रतिच्छाया दीख जाती है तो दूसरी ओर वे अपनी-अपनी मान्यता, अपने-अपने विश्वास की ओट में हर जायज़-नाजायज़ चलन को सही ठहराने की कुचेष्टा करते हैं। उनका यह सैलेक्टिव नैरेटिव या वैचारिक दोहरापन न सिर्फ़ उनकी साख़ को बट्टा लगाता है, अपितु उनकी नीयत पर भी सवाल खड़े करता है।धर्मनिरपेक्षता एवं सत्य के तमाम सवालों पर उनका एकपक्षीय एवं चयनवादी दृष्टिकोण जनसाधारण को व्यथित और विचलित करता रहा है।
मंगल-चाँद पर पहुँचते कदमों और घण्टों-महीनों की दूरियाँ पलों में मापते चमचमाते विमानों के दौर में क़बीलाई मानसिकता से चिपके रहने की समाज के एक तबक़े की जिद्द और जुनून सामान्य मानवी की समझ से परे है। सभ्य समाज ऐसे दुराग्रहों को छोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग तलाशता है।
अभी बक़रीद के अवसर पर उत्सव के नाम पर एक गाय को क्रेन से ऊपर ले जाकर ज़मीन पर पटकना और फिर उस हृदय-विदारक दृश्य पर तालियाँ बजाकर हर्षोल्लास प्रकट करना असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। बल्कि यों कहना चाहिए कि यह क्रूरता एवं बर्बरता की पराकाष्ठा है। आश्चर्य यह कि वहाँ उपस्थित बच्चे-बूढ़े-जवान, स्त्री-पुरुष सब उस दृश्य को देखकर रोमांचित और हर्षित हो रहे थे। ऐसी नृशंसता एवं बर्बरता को देखकर सहज ही यह सवाल उठता है कि क्या वहाँ उपस्थित समूह में से हरेक की संवेदना भोथरी हो चुकी थी? क्या जीव-हत्या के ऐसे उत्सव से मनुष्यता शर्मसार नहीं होती? बच्चों और स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से पाई जाने वाली करुणा और संवेदना का वहाँ उपस्थित समूह में ऐसा भयावह अभाव व अकाल क्या सभ्यता और मनुष्यता के एक नए संकट की ओर संकेत नहीं करता?
यह सवाल इसलिए और भी मौजूं हो जाता है कि क्यों गाय को ही क्रेन से ऊपर ले जाकर मरने-तड़पने के लिए ज़मीन पर पटका गया, क्या इसलिए कि उसमें करोड़ों लोगों की आस्था है? क्या ऐसे कुकृत्यों की खुली निंदा और मुखर किंतु अहिंसक विरोध नहीं होना चाहिए? ताकि सामाजिक सौहार्द्र एवं सद्भावना बची-बनी रहे? अच्छा तो यह होता कि इस विरोध का स्वर इस उत्सव को मनाने वाले समाज के भीतर से ही प्रारंभ हो, जिससे कि संपूर्ण देश-समाज में यह संदेश जाए कि ऐसी भीड़ सभी मतानुयायियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। बलि प्रतीकात्मक भी तो दी जा सकती है। बलि ही देनी है तो दुर्गुणों, कुप्रथाओं, कुरीतियों की दी जा सकती है। समय की माँग है कि उन्हें अपने भीतर से ही सुधारवादी, युगीन, मानवीय आंदोलन खड़ा करना चाहिए। सभ्य समाज में दकियानूसी रिवाज़ों और रवायतों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।यही सर्वसम्मत है, यही समयोचित है, यही सर्वसमावेशी है और यही धर्मानुकूल भी है।