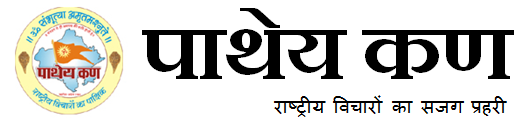राजनीति से साहित्य गायब लेकिन साहित्य में राजनीति भरपूर

डॉ. विकास दवे
 राजनीति से साहित्य गायब लेकिन साहित्य में राजनीति भरपूर
राजनीति से साहित्य गायब लेकिन साहित्य में राजनीति भरपूर
भारतीय समाज ने राजनीति को इतने निकृष्ट और घृणित विशेषण दे डाले हैं कि भारतीय समाज नेता शब्द को गाली की तरह उपयोग करने लगा है। नल का झगड़ा हो और झगड़े को सुलझाने या बीच-बचाव करने कोई आ जाए, तो दोनों झगड़ने वाले एक साथ कह उठते हैं- ज्यादा नेतागीरी सूझ रही है? कहने का तात्पर्य यह कि नेता वह जो दूसरों के फटे में टांग अड़ा सके। पर टांग तो सबसे अधिक हमारा यह बुद्धिमान साहित्यकार ही अड़ाता है। समाज का कोई भी क्षेत्र हो उसमें साहित्यकार यदि टांग ना अड़ाए, तो फिर वह बुद्धिजीवी कैसा? उस पर भी राजनीति को जब संज्ञा देने की बात आती है, तो इसी समाज के समझदार लोग उसे रक्कासा तक कह उठते हैं। हे भगवान! राजनीति यदि वेश्या है तो उस वेश्या के साथ समय बिताने वाला संपूर्ण लोकतांत्रिक समाज अपने आप को चरित्रवान कैसे कह लेता है? कहीं यह हम सबका चारित्रिक आत्मावलोकन तो नहीं है।
आज तक यह समीकरण समझ नहीं आया, पर बात तो दिल की है ना। दिल ने कहा और दिल ने सुना। हां यह बात अलग है कि जब दिल धीरे से फुसफुसाता है और दिल सुनता है, तो मन ही मन इसी राजनीति में भाग लेने वाले तत्कालीन नेताओं को अपने आसपास पाते ही यह सेल्फी लेने को मचल उठता है।
मंच पर नेताजी विराजमान हों और पीछे से जाकर यह पूछना कि आप चाय फीकी लेंगे या मीठी और अपने ही किसी चेले को मोबाइल से ठीक उसी क्षण क्लिक कर फोटो लेना और बाद में इंटरनेट मीडिया पर यह कहते हुए उस चित्र को डाल देना कि आज ही फलाने ढिकाने नेताजी से अमुक अमुक सीट पर प्रत्याशी फाइनल करते हुए, करना हमें खूब आता है। दरअसल, यह वही आदमी होता है जो नेताओं को 24 घंटे पानी पी-पीकर गालियां देता है और राजनीति को वेश्या से भी घृणित कहता है।
अब तुलसी बाबा तो रहे नहीं और ना रहे दिन भूषण के, जो साहित्य जगत के हम जैसे लोग यह कहने लगें कि संतन की सीकरी से क्या काम? और न ही हमारा साहस इतना बचा कि सीकरी की इच्छा के विरुद्ध धेले भर का सम्मान और बित्ते भर का अभिनंदन पत्र पा सकें। तभी तो हम अपना एक पैर देश की राजधानी और दूसरा पैर प्रदेश की राजधानी में रखने से गौरवान्वित अनुभव करने लगे।
एक समय था जब साहित्य राजनीति को सम्भालता था। नेहरू के लड़खड़ाते ही दिनकर द्वारा हाथ थाम कर उन्हें संभालना और कहना कि राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी, तब-तब साहित्य उसे थाम लेगा, इसका प्रमाण है?
किंतु आज तो साहित्य में राजनीति ही अधिक चल रही है, राजनीति में साहित्य नहीं। वार्ड का पार्षद हो या महापौर, विधायक, मंत्री हो या मुख्यमंत्री सब कुछ चलेगा। सांसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सियों की लगातार परिक्रमा करता हमारा साहित्य समाज राजनीति से दूर भागने का दावा करता कितना दयनीय लगने लगता है ना? काश साहित्य जगत राजनीति से दूर हो जाए तो साहित्य जगत का कल्याण तो हो ही जाए, राजनीति भी थोड़ी राहत की सांस ले। मगर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं।
(लेखक मप्र साहित्य अकादमी के निदेशक हैं)