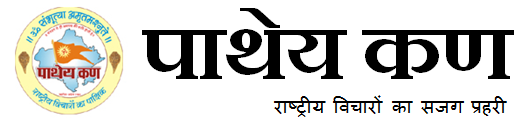एक साथ चुनाव आवश्यक क्यों?

हृदयनारायण दीक्षित
एक साथ चुनाव पर विचार करने वाली समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। इस रिपोर्ट का विरोध भी प्रारम्भ हो गया। एक साथ चुनाव का विषय देश के हित में है। लेकिन इस रिपोर्ट की सिफारिशों का विरोध भी हो रहा है। बताया जाता है कि यह रिपोर्ट 18000 पृष्ठ की है। इसे ठीक से पढ़े जाने और तथ्यों के विवेचन का काम बड़ा है। विरोध करने वाले भी संभवतः इस रिपोर्ट को पूरी तौर पर पढ़े बिना ही अपने निष्कर्ष निकाल रहे हैं। भारतीय जनतंत्र पूर्वजों के सचेत कर्मों का प्रसाद है। सभा समितियां ऋग्वैदिक काल में ही थीं। संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश तर्ज का संसदीय जनतंत्र अपनाया। अनेक संवैधानिक संस्थाएं गढ़ीं। केन्द्रीय स्तर पर संसद बनी। केन्द्र को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया। राज्य सरकारें विधानमण्डलों के समक्ष उत्तरदायी बनीं। संसद व विधानमण्डल के चुनाव के लिए निष्पक्ष निर्वाचन आयोग (अनु० 324) बना।
संविधान सभा में निर्वाचन आयोग के कृत्यों पर बहस हुई। आयोग को कर्मचारी अधिकारी देने का प्रश्न उठा। डॉ० आम्बेडकर ने कहा, ‘‘आयोग के पास कम काम होगा।” शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा कि, ‘‘संविधान में निर्धारित नहीं है कि अमेरिकी तर्ज पर यहाँ 4 वर्ष में निर्वाचन अवश्य होगा। संभव है कि केन्द्र व राज्यों के निर्वाचन एक साथ न हों। तब हर समय कहीं न कहीं निर्वाचन होता रहेगा।” उनकी आशंका सच निकली। सम्प्रति भारत चुनाव में व्यस्त देश है। कभी लोकसभा चुनाव तो बहुधा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव व नगर निकाय निर्वाचन भी अक्सर होते रहते हैं। नीति आयोग ने लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इसी विचार के हैं। 2014 के चुनाव में भाजपा ने भी घोषणा पत्र में यही विचार व्यक्त किया था।
लगातार चुनाव व्यस्तता राष्ट्रीय विकास में बाधा है। अलग-अलग चुनावों से प्रशासनिक तंत्र की व्यस्तता बनी रहती है। चुनावी आचार संहिता के कारण विकास कार्य रुकते हैं। अरबों का खर्च भी होता है। साथ साथ चुनाव का विचार स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से अपील की थी। कहा था, ‘‘एक साथ चुनाव से दलों का नुकसान होगा। हमें भी नुकसान होगा लेकिन इसे संकीर्ण राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।”
1951-52 में पहली लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। 1967 तक दोनों के चुनाव साथ-साथ हुए थे। 1968 से यह क्रम टूट गया। दरअसल संविधान निर्माताओं ने सरकारों का कार्यकाल नहीं सुनिश्चित किया। यहाँ सरकारों का जीवन संसदीय बहुमत की डोर से बंधा हुआ है। डॉ० आम्बेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था कि सरकारी जवाबदेही को स्थिरता (कार्यकाल) की तुलना में ऊपर रखा गया है। सदन में सरकारों की संवैधानिक जवाबदेही है। इस आधारभूत सिद्धांत में सरकारों का कार्यकाल अनिश्चित है। यहाँ बहुमत स्थाई नहीं होता। दल बदल प्राविधान में भी छेद किए गए। थोक दल बदल को दल टूट कहा गया। अनेक सरकारें अल्प मृत्यु की शिकार हुईं। साथ साथ चुनाव का क्रम भंग हो गया।
साथ साथ चुनाव से राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय संदर्भों से जुड़ने की ओर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय दलों की दृष्टि राष्ट्रीय होगी। लेकिन कुछ दलों की चिन्ता बड़ी है। बीते कुछेक वर्षों में राष्ट्रीयता का भाव देशव्यापी हुआ है। माकपा, भाकपा जैसे वामपंथी दल स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा का दल बताते हैं लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र राज्यस्तरीय भी नहीं बचा। चुनाव आयोग ने बेशक केन्द्रीय विधि मंत्रालय के एक संदर्भ के जवाब में दोनों चुनाव एक साथ कराने पर बहुत पहले ही सहमति व्यक्त की थी लेकिन सभी दलों की सहमति प्राप्त करना आसान नहीं। कुछेक दल वर्तमान स्थिति को ठीक मानते हैं और चुनाव अलग अलग ही चाहते हैं।
लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार आदर्श है। लोकसभा का चुनाव अलग व देश की सभी विधानसभाओं के चुनाव अलग से कराने का विचार भी आया था। कुछ दल इस विचार को उचित मान सकते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। संशोधन में केन्द्र व राज्य सरकारों को सुनिश्चित कार्यकाल देना होगा। सदन में बहुमत खो जाने की स्थिति में सरकारी कार्यकाल की समस्या का निराकरण आवश्यक होगा। दसवीं अनुसूची के अनुसार दल से भिन्न मतदान के कारण सदन की सदस्यता खो जाने की विधि प्रवर्तन में है। मूलभूत प्रश्न किसी भी कारण से सदन में बहुमत खो चुकी सरकार को पूरा कार्यकाल देने की नई व्यवस्था का है। क्या वैकल्पिक सरकार बनाने का अधिकार संसद या विधानसभा को दिया जा सकता है? क्या हमारा दलतंत्र स्थिर कार्यकाल और संवैधानिक जवाबदेही को एक साथ चला सकता है? क्या संवैधानिक जवाबदेही को छोड़कर स्थिरता को ही अपनाया जा सकता है? अमेरिका में ऐसा ही है।
प्रश्न ढेर सारे हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर संविधान संशोधन और वैधानिक नैतिकता से ही जुड़ा हुआ है। डॉ० आम्बेडकर ने संविधान सभा में इतिहासकार ग्रोट को उद्धृत किया था। ‘वैधानिक नैतिकता‘ का अर्थ संविधान और उसकी संस्थाओं के प्रति निष्ठाभाव है। ग्रोट ने लिखा है कि समाज की वैधानिक नैतिकता ही विधान की शक्ति है। भारत का जनसामान्य विधान का आदर करता है लेकिन दलतंत्र में वैधानिक नैतिकता का अभाव है। इसलिए सरकारें बहुधा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पातीं। तब लोकसभा और विधानसभा के मध्यावधि चुनाव का कोई विकल्प नहीं होता। संसदीय जनतंत्र का मुख्य उपकरण दलतंत्र है। जनतंत्र खूबसूरत विचार है। दलतंत्र ही इसे गतिशील बनाता है। समाज व्यवस्था निरंतर परिवर्तनशील है। लेकिन राजनैतिक व्यवस्था में राजनैतिक सुधार की गति उत्साहवर्द्धक नहीं है। दलतंत्र प्रतिपल चुनाव चिन्तन में ही व्यस्त रहता है। चुनाव चिन्तन को राष्ट्रचिन्तन के खूंटे से बांधना ही होगा। साथ साथ चुनाव एक राष्ट्र हितैषी प्रगतिशील वैकल्पिक विचार है। 1952 से लेकर 1967 तक यही हुआ था, तब कोई पहाड़ नहीं टूटा तो अब इसे अपनाने में कठिनाई क्या है?
सभी राजनैतिक दलों को खुले मन से विचार करना चाहिए। लोकसभा, विधानसभा के साथ पंचायती व नगरीय संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव पर भी। सभी एक साथ नहीं तो विधानसभा के साथ पंचायतों व नगर पंचायतों के चुनावों को जोड़कर विचार करना चाहिए। कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी। हर समय चुनाव ही चुनाव का तनाव समाज नहीं झेल सकता और न ही चुनाव संचालन में खर्च होने वाली भारी धनराशि का बोझ ही। आमजन भी ऐसी राजनीति से ऊबे हुए हैं। इसलिए राजनीति को दीर्घकालिक राष्ट्रनिर्माण के लक्ष्य से जोड़ना चाहिए। चुनावी जीत हार के अल्पकालिक लक्ष्य से नहीं। दल या नेता स्थाई नहीं होते। राष्ट्र स्थाई सत्ता है। सभी सामाजिक, राजनैतिक या संवैधानिक संस्थाएं राष्ट्र का ही विस्तार हैं। राष्ट्र के लिए ही हैं। एक साथ चुनाव राजनैतिक सुधार है। राजनैतिक सुधार लोकतंत्र को गुणवान बनाते हैं। व्यापक राजनैतिक सुधारों का कोई विकल्प नहीं।
साभार