औपनिवेशिक गुलामी का बोझ कब तक?

मुरारी गुप्ता
 औपनिवेशिक काल उन सभी देशों के लिए शोषण और अत्याचार का कालखंड था, जहां यूरोपियन देशों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। सवाल है कि हम क्यों अभी तक भारत में ब्रिटिश और मुगलों की गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिह्नों और ढो रहे हैं? यह सही समय है जब हम गुलामी के प्रतीक चिह्नों, मूर्तियों, कानूनों को ख़त्म कर देश को मानसिक गुलामी की दासता से मुक्त करें, ताकि नई पीढ़ी एक स्वाभिमानी, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र में सांस ले सकें।
औपनिवेशिक काल उन सभी देशों के लिए शोषण और अत्याचार का कालखंड था, जहां यूरोपियन देशों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। सवाल है कि हम क्यों अभी तक भारत में ब्रिटिश और मुगलों की गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिह्नों और ढो रहे हैं? यह सही समय है जब हम गुलामी के प्रतीक चिह्नों, मूर्तियों, कानूनों को ख़त्म कर देश को मानसिक गुलामी की दासता से मुक्त करें, ताकि नई पीढ़ी एक स्वाभिमानी, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र में सांस ले सकें।
अमरीका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस प्रताड़ना में मौत ने अमरीका सहित पूरी दुनिया को झिंझोड़कर रख दिया है। ‘श्वेत ही श्रेष्ठ हैं’ की गुलाम मानसिकता से बाहर निकलने में संसार को लगता है अभी काफी समय लगेगा। लेकिन इस घटना के साथ एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है वह है दुनियाभर में लोग ‘श्वेत ही श्रेष्ठ है’ की मानसिकता का प्रचार प्रसार करने वाली यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक नीति के अवशेषों को भी समाप्त कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अमरीका के रिचमंड शहर में यूरोप के लिए अमरीका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस की मूर्ति को तोड़कर झील में फेंक दिया। इसी तरह लंदन में भी गुलामों के व्यापारी रहे रॉबर्ट मिलीगन की मूर्ति को हटा दिया गया।
औपनिवेशिक काल उन सभी देशों के लिए शोषण और अत्याचार का कालखंड था, जहां यूरोपीयन देशों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इस कालखंड की मानवीय अत्याचारों, आर्थिक शोषण और धार्मिक उत्पीड़न से भरी घटनाएं यूरोपीय देशों को शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त हैं। फिर क्यों नहीं उन औपनिवेशिक प्रतीक चिह्नों को उखाड़ फेंका जाए, जो अभी भी नागरिकों में मानसिक गुलामी को जिंदा रखती हैं। क्या मानवता का ढोंग करने वाले उन यूरोपीय देशों को मानवता के खिलाफ रचे गए औपनिवेशिक शोषण के लिए सभी पीड़ित देशों से माफी नहीं मांगनी चाहिए?
दुर्भाग्य से भारत में ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी के प्रतीक चिह्न और अव्यवहारिक कानून अभी भारतीय व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं। आखिर कब तक? वर्ष 2015 में ब्रिटेन मे आयोजित एक वाद विवाद में हिस्सा लेते हुए भारतीय सांसद और लेखक शशि थरूर ने भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता को लेकर कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने बताया था कि अठारवीं सदी की शुरुआत में विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 23 फ़ीसदी थी। उपनिवेश काल में ब्रिटिश हुकूमत ने बेरहमी से भारत का शोषण किया और तीन करोड़ भारतीयों की भूख की वजह से मौत हो गई थी। सवाल है कि हम क्यों अभी तक भारत में ब्रिटिश और मुगलों की गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिह्नों को ढो रहे हैं? क्या हमें भी ऐसे औपनिवेशिक प्रतीकों को उखाड़ कर नहीं फेंक देना चाहिए जिनसे गुलामी की बू आती है? इनमें से एक है राष्ट्रकुल की सदस्यता और कॉमनवैल्थ गेम्स। भारत में अनेक विद्वानों का मत है कि हमें अब कामनवेल्थ की सदस्यता से हट जाना चाहिए। विश्व राजनीति में अब भारत का महत्व ब्रिटेन से भी कहीं अधिक है लेकिन मानसिक दासता ऐसी बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं। राष्ट्रकुल में रहने से भारत को सबसे बड़ा तो भाषिक नुकसान है। भारत में अंग्रेजी के दबदबे के पीछे राष्ट्रकुल का प्रभाव ही है। अंग्रेजी ने पूरे देश की रग-रग में हीनता की ग्रंथि पैदा कर दी है।
राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत से ही ब्रिटिश राज की मंशा समझ में आती थी। 1891 में पहली बार इन खेलों का प्रस्ताव रखा गया था ताकि ब्रिटिश कॉलोनी के देश एक दूसरे को जान सकें। रेवरेन्ड एसले कूपर ने द टाइम्स अखबार में एक लेख लिखा जिसमें प्रस्ताव रखा गया कि हर चार साल में इस तरह का एक आयोजन किया जाए ताकि ब्रिटिश राज की सद्भावना के बारे में लोग जानें और समझें। ब्रिटिश राज की सद्भावना के बारे में पढ़ना कितना हास्यास्पद है। क्या राष्ट्रमंडल खेलों का स्वरूप नहीं बदला जाना चाहिए। भारत को इसकी शुरुआत करनी चाहिए।
इसी तरह भारतीय विमानों पर लिखा भारतीय विमानसेवा का कोड-वीटी (वायसराय टेरिटरी) भी ब्रिटिश गुलामी का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) हर देश की विमान सेवा को एक सिग्नल कोड प्रदान करता है। हालांकि वर्ष 2017 में इस बारे में राज्यसभा में उठे सवाल के जबाव में सरकार ने कहा था कि इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन हम ऐतिहासिक तथ्यों को नहीं झुठला सकते। भारतीय विमान सेवाओं को यह कोड 1929 में मिला था, जब यहां ब्रिटिश राज था और पूरा देश वायसराय के अधीन था। स्वतंत्रता के बाद भी हमने इसे ढोते रहने का निर्णय किया और दुर्भाग्य से अभी तक ढो रहे हैं, जबकि चीन, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका ने अपने अपने कोड बदल लिए हैं। यद्यपि भारत ने इसके लिए प्रयास भी किए लेकिन तकनीकी कारणों से अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। फिर भी हमें गुलामी के इस प्रतीक चिह्न से मुक्ति का रास्ता निकालना ही चाहिए।
वर्तमान केंद्र सरकार ने हजारों की संख्या में ब्रिटिश काल में बने कानूनों को या बदल दिया है, या रद्द कर दिया है तथापि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत से शब्द और कार्यप्रणाली को हम अब तक ढो रहे हैं। इन्हें धीरे धीरे समाप्त कर हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलन में कलेक्टर, सिविल लाइंस और सर्किट हाउस ऐसे शब्द हैं, जिन्हें प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे शब्दों को समाप्त कर देना चाहिए जो समाज में वर्गभेद पैदा करते हों। प्रमोद के नायर की पुस्तक ‘द ब्रिटिश राजः कीवर्ड्स’ के अनुसार ब्रिटिश काल में वारेन हेंस्टिंग्ज ने 1770 में राजस्व संग्रह के लिए कलेक्टर का पद स्थापित किया था। लेकिन समय, देशकाल और जिम्मेदारियां बदलने के बाद आज भी कलेक्टर पद और शब्दावली को ढोया जा रहा है और समाज में स्टेटस का प्रतीक बन गया है। हर छोटे-बड़े शहर में मौजूद सिविल लाइंस क्षेत्र विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए सुरक्षित होते हैं। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश अधिकारियों के आवास के लिए सिविल लाइन्स क्षेत्र बनाए गए थे। इसी तरह हर राज्य में मौजूद जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के प्रवास के दौरान रुकने के लिए बने सरकारी आवास- सर्किट हाउस भी ब्रिटिश कालीन सर्किट जजों के आवास के लिए बने थे। लेकिन उनका नाम भी नहीं बदल सके हैं।
कुछ प्रतीक चिह्न ऐसे हैं जो भारत को चिढ़ाते हैं। मुम्बई के विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया लेकिन राष्ट्रध्वज से ऊपर अंग्रेजों की महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा अभी तक लगी हुई है। यह गर्व का विषय तो बिलकुल नहीं हो सकती है। माना कि यह भवन अंग्रेजों के कालखंड में बना था, लेकिन इसमें लगने वाला धन और मानवश्रम भारत का था।
कुछ शहरों के नाम भी हमें चिढ़ाते हैं और अत्याचार के कालखंड का स्मरण करवाते हैं। उत्तराखंड जैसी देवभूमि पर दंगे भड़काने वाले अंग्रेज अधिकारी लेंसडाउन के नाम पर शहर बसा है। बेशकीमती कोहिनूर हीरे के लुटेरे डलहौजी के नाम पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में डलहौजी शहर बसा है। ब्रिटिश सेना के अत्याचारी अधिकारी मैक्लॉडगंज के नाम पर धर्मशाला जिले में एक शहर बसा है। पहले पुर्तगाली लुटेरे वास्कोडिगामा के नाम पर गोवा में एक शहर बसा है। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि नाम बदलने से क्या इतिहास बदला जा सकता है? इसका जबाव है हां। नाम बदलने से नागरिकों का सोचने का तरीका बदल जाता है। मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी से ज्यादा भयावह होती है, क्योंकि शारीरिक गुलामी से केवल एक पीढ़ी जबकि मानसिक गुलामी से कई पीढियां खत्म हो जाती है। यह सही समय है जब हम गुलामी के प्रतीक चिह्नों, मूर्तियों, कानूनों को ख़त्म कर देश को मानसिक गुलामी की दासता से मुक्त करें, ताकि नई पीढ़ी एक स्वाभिमानी, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र में सांस ले सके।
(लेखक भारतीय सूचना सेवा में कार्यरत हैं)
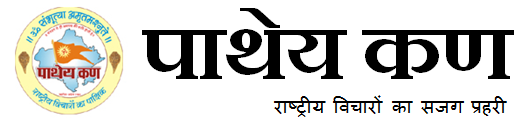

बहुत अच्छा, विचारोत्तेजक लेख! साधुवाद, मुरारी जी!