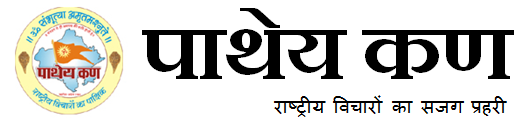चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता की कमी

प्रमोद भार्गव
 चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता की कमी
चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता की कमी
देश में चिकित्सकों की कमी के बावजूद चिकित्सा शिक्षा में स्नातकोत्तर कक्षाओं में 1456 सीटें खाली रह जाना चिंता का विषय है। ये सीटें राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट पीजी) के बाद खाली रही हैं। इसे लेकर शीर्ष न्यायालय ने भी नाराजगी जताते हुए चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) को कड़ी फटकार लगाई थी। साथ ही हिदायत दी थी कि एक भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए विशेष परामर्श के बाद सीटें भरी जाएं। किंतु अगली सुनवाई में न्यायालय ने केंद्र सरकार और एमसीसी के फैसले को सही मानते हुए कहा कि इसे मनमाना निर्णय नहीं कह सकते, क्योंकि पढ़ाई की गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं तो लोक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अतएव एमसीसी का निर्णय जन-स्वास्थ्य के हित में है। इस परिप्रेक्ष्य में विडंबना है कि एक तरफ तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी के चलते बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गईं, दूसरी तरफ कई प्रतिभावान छात्र जटिल विषयों में पीजी करना ही नहीं चाहते हैं।
जब कोई एक प्रचलित व्यवस्था संकट में आती है, तो कई संदेहास्पद सवालों का उठना स्वाभाविक है। क्योंकि मेडिकल चिकित्सा के पीजी पाठ्यक्रमों में खाली सीटें रह जाने में छात्रों की रुचि नहीं होना भी है। इस परिप्रेक्ष्य में 2015-16 में शल्य चिकित्सक हृदय (कार्डियक) में 104, हृदयरोग विशेषज्ञ 55, बालरोग विशेषज्ञ 87, प्लास्टिक सर्जरी 58, स्नायु-तंत्र विशेषज्ञ (न्यूरोलॉजिस्ट)-48 और स्नायुतंत्र शल्यक्रिया विशेषज्ञों की भी 48 सीटें रिक्त रह गई थीं। इस कमी के दो कारण गिनाए गए थे, एक तो यह कि इन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं मिले, दूसरे, पीजी के लिए जो योग्य विद्यार्थी मिले भी, उन्होंने इन पाठ्यक्रमों में पढ़ने से मना कर दिया। अब 1456 सीटें खाली रहने के पीछे योग्य विद्यार्थियों का उपलब्ध नहीं होना बताया है। आखिर क्या कारण हैं कि चिकित्सा शिक्षा में अनेक सुविधाएं बढ़ जाने के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा पा रही है?
ऐलौपैथी चिकित्सा विषेशज्ञों का मानना है कि आज के विद्यार्थी उन पाठ्यक्रमों में अध्ययन करना नहीं चाहते, जिनमें विशेषज्ञता प्राप्त करने में लंबा समय लगता है। इसके उलट वे ऐसे पाठ्यक्रमों में दक्षता हासिल करना चाहते हैं, जहां जल्दी ही विशेषज्ञता की उपाधि प्राप्त कर धन कमाने के अवसर मिल जाते हैं। गुर्दा, नाक, कान, दांत, गला रोग एवं विभिन्न तकनीकी जांच विषेशज्ञ 35 साल की उम्र पर पहुंचने के बाद शल्यक्रिया शुरू कर देते हैं, जबकि हृदय और तांत्रिका-तंत्र विशेषज्ञों को यह अवसर 40-45 साल की उम्र बीत जाने के बाद मिलता है। साफ है, दिल और दिमाग का मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए इनमें लंबा अनुभव भी आवश्यक है। लेकिन यह समस्या अनवरत बनी रही तो भविष्य में इन रोगों के उपचार से जुड़े चिकित्सकों की कमी आना तय है। इस व्यवस्था में कमी कहां है, इसे ढूंढना और फिर उसका निराकरण करना तो सरकार और ऐलौपैथी शिक्षा से जुड़े लोगों का काम है, लेकिन फिलहाल इसके कारणों की पृष्ठभूमि में भारतीय चिकित्सा परिषद को निरस्त कर ‘राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद‘ बनाना और चिकित्सा शिक्षा का लगातार महंगा होते जाना तो नहीं?
2016 में एमएमसी अस्तित्व में लाने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है। आरंभ में इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारना, इस पेशे को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के अनैतिक गठजोड़ तोड़ता था। लेकिन जब एमएमसी कानून में आया तो इसमें प्रमुख लोच रहा कि आयुर्वेद, हैम्योपैथी और यूनानी चिकित्सक भी सरकारी स्तर पर (ब्रिज कोर्स) करके वैधानिक रूप से ऐलौपेथी चिकित्सा करने के हक पा लेते हैं। यह क्रम अनेक स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से देशभर में चल भी पड़ा है। इस पाठ्यक्रम का शुल्क 25 हजार रुपए है। हालांकि अभी भी इनमें से ज्यादातर चिकित्सक बेखटके एलौपैथी की दवाएं लिखते हैं, किंतु यह व्यवस्था अभी गैर-कानूनी है और जिले के सरकारी स्वास्थ्य विभाग के कदाचरण पर चलती है। संभव है, इस विरोधाभास को समाप्त करने और गैर-कानूनी चिकित्सा को कानूनी बना देने की दृष्टि से ही इस कानून में सेतु-पाठ्यक्रम की सुविधा देकर इन्हें ऐलोपैथी चिकित्सा की वैधता प्रदान करना रहा हो?
लेकिन क्या किसी साधारण ऑटो-टैक्सी लाइसेंसधारी चालक को आप कुछ समय प्रशिक्षण देकर हवाई जहाज चलाने की अनुमति दे सकते हैं? दरअसल उपचार की हरेक पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है और सैकड़ों साल के प्रयोग व प्रशिक्षण से वह परिपूर्ण हुई है। सबकी पढ़ाई भिन्न है। रोग के लक्षणों को जानने के तरीके भिन्न हैं, और दवाएं भी भिन्न हैं। ऐसे में चार-छह माह की एकदम से भिन्न पढ़ाई करके कोई भी वैकल्पिक चिकित्सक ऐलौपैथी का मास्टर नहीं हो सकता। ऐसा करने से आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का भी भट्ठा बैठ सकता है क्योंकि ऐलौपैथी में कमाई असीमित है और इसके इलाज से तत्काल राहत भी मिलती है, ऐसे में वैकल्पिक चिकित्सक अपनी मूल पद्धति से उपचार क्यों करेंगे? वैसे भी रूस, यूक्रेन और अन्य देशों से जो छात्र एमबीबीएस करके आ रहे हैं, वे किसी रोग विशेष की विशेषज्ञता नहीं होने के बावजूद, रोग विशेष का इलाज धड़ल्ले से कर रहे हैं।
एमबीबीएस और इससे जुड़े विषयों में पीजी में प्रवेश बहुत कठिन परीक्षा है। एमबीबीबीएस में कुल 67,218 सीटें हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1 हजार की जनसंख्या पर एक डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य मानता है, लेकिन हमारे यहां यह अनुपात 62:1000 है। 2015 में राज्यसभा में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया था कि 14 लाख ऐलौपैथी चिकित्सकों की कमी है। किंतु अब यह कमी 20 लाख के पार चली गई है। इसी तरह 40 लाख नर्सों की कमी है। सरकारी जिला अस्पताल से लेकर अन्य सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच उपकरणों की तो भरमार हो गई है, लेकिन तकनीशियन की पूर्ति उपकरणों के अनुपात में नहीं हुई।
एमबीबीबीएस शिक्षा के साथ कई तरह के खिलवाड़ हो रहे हैं। कायदे से उन्हीं छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलना चाहिए, जो सीटों की संख्या के अनुसार नीट परीक्षा से चयनित हुए हैं। लेकिन स्थिति यह है कि जो छात्र दो लाख से भी ऊपर की रैंक में है, उसे भी धन के बूते प्रवेश मिल जाता है। यह स्थिति इसलिए बनी हुई है, क्योंकि जो मेधावी छात्र निजी कॉलेज का शुल्क अदा करने में सक्षम नहीं हैं, वह मजबूरी वश अपनी सीट छोड़ देते हैं। बाद में इसी सीट को निचली श्रेणी में स्थान प्राप्त छात्र खरीदकर प्रवेश पा जाते हैं। इस सीट की कीमत 60 लाख से एक करोड़ तक होती है। इससे होता यह है कि जो छात्र एमबीबीबीएस में प्रवेश की पात्रता नहीं रखते हैं, वे अपने अभिभावकों की नैतिक/ अनैतिक कमाई के बूते इस पवित्र और जिम्मेवार पेशे के पात्र बन जाते हैं। ऐसे में इनकी अपने दायित्व के प्रति कोई नैतिक प्रतिबद्धता नहीं होती है। पैसा कमाना ही इनका एकमात्र लक्ष्य रह जाता है। अपने बच्चों को हर हाल में मेडिकल और आईटी कॉलेजों में प्रवेश की यह महत्वाकांक्षा रखने वाले पालक यही तरीका अपनाते हैं। देश के सरकारी कॉलेजों का एक साल का शुल्क महज 4 लाख है, जबकि निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में यही शुल्क 64 लाख है। यही धांधली एनआरआई और अल्पसंख्यक कोटे के छात्रों के साथ बरती जा रही है। एमडी में प्रवेश के लिए निजी संस्थानों में जो प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र और अनुदान आधारित सीटें हैं, उनमें प्रवेश शुल्क की राशि 2 करोड़ से 5 करोड़ है। बावजूद सामान्य प्रतिभाशाली छात्र के लिए एमएमबीबीएस परीक्षा कठिन बनी हुई है।
एनएमसी कानून में संस्था को न्यायालय की तरह विवेकाधीन अधिकार भी दिए गए हैं। इसे ये अधिकार भी हैं कि यह चाहे तो उन चिकित्सकों को भी मेडिसन और शल्यक्रिया की अनुमति दे सकती है, जिन्होंने लाइसेंसिएट परीक्षा पास नहीं की है। जबकि एमबीबीबीएस पास छात्रों को भी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले यह परीक्षा पास करनी होती है। जो विद्यार्थी विदेश से ऐलौपैथी चिकित्सा की डिग्री लेकर भारत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यह एनएमसी के विवेक पर निर्भर होगा कि उसे प्रैक्टिस करने की अनुमति दे अथवा नहीं? यही वह झोल है, जो भ्रष्टाचार को पनपने के छेद खोलते हैं।
एक ओर तो हम आरक्षण के नाम पर जाति आधारित योग्यता व अयोग्यता का ढिंढोरा पीटते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस कानून के माध्यम से निजी महाविद्यालयों को 60 प्रतिशत सीटें प्रबंधन की मनमर्जी से भरने की छूट दे देते हैं। अब केवल 40 प्रतिशत सीटें ही प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। साफ है, प्रबंधन उसके अधिकार क्षेत्र में आई 60 प्रतिशत सीटों की खुल्लम-खुल्ला नीलामी करेगा? परिणामस्वरूप इस कानून का असर पीजी सीटें खाली रह जाने के रूप में अब स्पष्ट दिखने लगा है। यह स्थिति देश की भावी स्वास्थ्य सेवा को संकट में डालने के संकेत हैं। दरअसल चिकित्सा शिक्षा में ऐसे सुधार दिखने चाहिए थे, जो इसमें धन से प्रवेश के रास्तों को बंद करते। श्रीलाल शुक्ल अपने प्रसिद्ध उपन्यास ‘राग दरबारी‘ में बहुत पहले लिख गए हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली आम रास्ते पर पड़ी वह बीमार कुतिया है, जिसे लतियाते तो सब हैं, परंतु इलाज कोई नहीं करता।