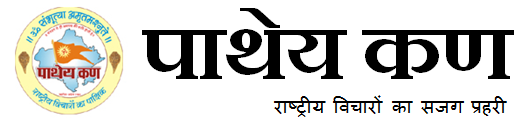विकास दुबे एनकाउंटर से उपजे सवाल

प्रणय कुमार

विकास दुबे एनकाउंटर ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिये हैं। क्या वास्तव में दोषियों को दंड और निर्दोषों को न्याय देने में हमारा न्याय-तंत्र विफल रहा है? आँकड़े बताते हैं कि लगभग साढ़े तीन करोड़ मुक़दमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।
विकास दुबे का एनकाउंटर सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज, न्याय, पुलिस और प्रशासन व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान भी है। नहीं तो क्या वजह है कि समाज का बड़ा तबका ऐसे तात्कालिक न्याय पर जश्न मनाने लगता है। क्या हमारा न्याय-तंत्र खोखला हो चला है? क्या उस पर से लोगों का विश्वास उठ चला है? क्या विलंब से मिलने वाले न्याय के कारण आम लोगों का धैर्य चुक गया है? क्या व्यवस्था के छिद्रों का लाभ उठाने वाले रसूखदारों के कारण आम लोगों की यह धारणा बन चुकी है कि न्याय भी भेदभाव करती है? क्या न्याय सबके लिए समान और सुलभ नहीं है? क्या दोषियों को दंड और निर्दोषों को न्याय देने में हमारा न्याय-तंत्र विफल रहा है? ये केवल सवाल भर नहीं है। इसकी पुष्टि हमारे सामने लंबित मुकदमों पहाड़ करता है। आँकड़े बताते हैं कि लगभग साढ़े तीन करोड़ मुक़दमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।
अगर अन्य देशों से तुलना करें तो चीन में 99.9, अमेरिका में 68, ब्रिटेन में 80, इजरायल में 88 प्रतिशत मामलों में न्याय मिल पाता है। लेकिन हमारे यहां न्याय मिलने का औसत दर मात्र 40 प्रतिशत ही है। बल्कि यौन उत्पीड़न के मामलों में न्याय मिल पाने का दर तो मात्र 18 प्रतिशत ही है (स्रोत-जी न्यूज़) दोषियों को सज़ा और निर्दोषों को न्याय देने के मामले में हमारा देश विश्व में सत्तरवें स्थान पर आता है।
यह बहुत विचारणीय सवाल है कि आखिर क्यों हर एनकाउंटर के पश्चात आम जनता में जश्न का माहौल होता है और हर सरकार एवं पुलिस-विभाग इसे अपनी बड़ी क़ामयाबी के रूप में प्रचारित करती है। राजनैतिक दल इन एनकाउंटरों को चुनावों में भुनाने का प्रयास करते हैं। क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि ये अपराधी बिना राजनीतिक एवं व्यवस्थागत संरक्षण के फल-फूल रहे हैं।
इसके साथ समाज के सबसे बड़ी चिंता अपराधों के जातीयकरण की है। चाहे राजस्थान के आनंदपाल की बात हो या फिर विकास दुबे की। आखिर क्यों कुछ लोग अपराधियों को समाज के मसीहा के तौर पर स्थापित करने में जुट जाते हैं? पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि विभिन्न जातियों के कथित तौर पर अपराधी-नायक बने बैठे हैं। अपराधियों में नायकत्व की छवि तलाशना सभ्य समाज के पतन की पराकाष्ठा है।
जब सामाजिक आदर्श छीजने लगे, स्वार्थ हावी होने लगे, समाज में जातीय विभाजन की खाई गहरी होती चली जाय, तभी ऐसा संभव है। जब किसी अपराधी को जातीय-गौरव का प्रतीक-पर्याय बना दिया जाता है तो उसकी सज़ा आने वाली पीढ़ियाँ भुगतती हैं। कालांतर में या तो उन्हें उस पहचान-प्रतीक से बेमतलब जोड़ दिया जाता है या युवा-अपरिपक्व मन उन अपराधियों-जैसा बनकर नाम कमाने की वैसी ही हसरतें पालने लगता है।
हालात तब और भी बुरे हो जाते हैं जब सिनेमा जैसे माध्यम इन अपराधियों को महिमामंडित करते हुए उन्हें प्रदर्शित करता है। होना तो यह चाहिए कि समाज को अपराधी से उसका सरनेम छीन लेना चाहिए। उसे शुरुआत से ही बहिष्कृत कर देना चाहिए। और सार्वजनिक घोषणा कर देनी चाहिए कि अमुक अपराधी से उस समाज का कोई व्यवहार नहीं है। इससे पूरे समाज में एक स्वस्थ वातावरण निर्मित होगा।
समय आ गया है कि हम एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने के स्थान पर आपराधिक प्रवृति को रोकने के समाधान के लिए सार्थक एवं ठोस पहल करें| हमें अपनी संततियों, किशोरों-युवाओं को समझाना होगा कि अपराधियों की कोई जाति, मज़हब या ईमान नहीं होता। अपराधी की पहचान केवल उसका अपराध है।
समाज में बढ़ते अपराध और अपराधियों के फलते-फूलते साम्राज्य पर अंकुश लगाने के लिए हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था में भी आमूल-चूल सुधार करना होगा। अनावश्यक विलंब को टालकर समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना होगा। ट्रिब्यूनल, फ़ास्ट ट्रैक, लोक-अदालत, ग्राम्य न्यायालय आदि का गठन कर लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना होगा। अपील और तारीख़ों की संख्या निश्चित करनी होगी और अपराध की प्रकृति के आधार पर ज़मानत की प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल या जटिल बनाना होगा। न्यायाधीशों और न्यायालयों की संख्या बढ़ानी होगी। न्याय-तंत्र में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार को दूर करना होगा। जजों की भी जवाबदेही तय करनी होगी, नियुक्ति से लेकर निर्णय तक पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी, विधायिका-कार्यपालिका-न्यायपालिका के बीच बेहतर ताल-मेल स्थापित करना होगा और इन सबसे अधिक जन-जागृति एवं जन-भागीदारी को प्रोत्साहित कर न्याय-तंत्र पर आम नागरिकों के विश्वास को पुनः बहाल करना होगा।
(ये लेखक के निजी विचार हैं)