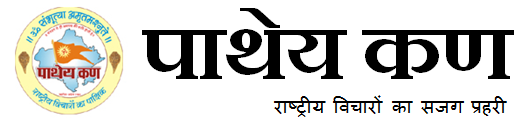विनाशपर्व – अंग्रेजों ने नष्ट की भारत की उन्नत चिकित्सा व्यवस्था / 3

प्रशांत पोळ
सन् 1796 में डॉ. एडवर्ड जेनर (1749 – 1823) ने गाय के चेचक के दानों से चेचक का टीका बनाने की खोज की, चूंकि यह एक अंग्रेज डॉक्टर का खोजा हुआ तरीका था, अतः इस पर तत्काल विश्वास किया गया और भारत में उसे तत्काल लागू किये जाने की सिफारिश की गई ताकि अंग्रेज सिपाहियों की स्वास्थ्य रक्षा हो सके। इन टीकों को बर्फ के बक्सों में रखकर भारत लाया जाता था फिर उससे भारतीयों को चेचक के टीके लगवाये जाते थे। टीका लगाने का तरीका ठीक वही था जो हमारे लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस पद्धति का नाम पडा वैक्सीनेशन। इसके लिये बड़ी सख्ती करनी पड़ती थी क्योंकि यदि किसी भारतीय ने अंग्रेजी टीका नहीं लगवाया तो अंग्रेज डॉक्टरों का डर था कि आगे उसे चेचक निकलेंगे और वह महामारी फैलाने का एक माध्यम बनेगा। आरंभ काल में अंग्रेजी टीका लगाने के तरीके काफी दुखद होते थे। उनकी जख्में बड़ी होती थीं और बच्चे या बूढ़े उन्हें लगवाने से डरते और रोते पीटते थे। ‘जेनर विधि’ के अर्न्तगत वैक्सीनेशन का टीका लगवाने पर उस जगह घाव हो जाता था और बुखार भी आता था, लेकिन चेचक के दाने नहीं उभरते थे, जैसा कि देसी वेरिओलेशन की प्रणाली में निकलते थे। कई बार टीके का बुखार तीव्र होकर मृत्यु भी हो जाती जिस कारण भारतीयों का विरोध अधिक था।
अंग्रेजों को यह लग रहा था कि जब तक काशी के ब्राह्मणों के शिष्य अपना वेरिओलेशन (टीकाकरण) का कार्यक्रम कर रहे हैं, तब तक उनके लिये चुनौती कायम रहेगी। उसे रोकने के लिए देशी तरीके को अशास्त्रीय करार दिया गया और शीतला माता’ का टीका लगाने वाले ब्राह्मणों को जेल भिजवाया जाने लगा। तब ब्राह्मणों ने अपनी विद्या गांव-गांव के, सुनार और नाइयों को सिखाई। इस प्रकार उनके माध्यम से भी यह देसी पद्धति से टीके लगाने का काम कुछ वर्षों तक चलता रहा। जिन सुनार या नाइयों को यह विद्या सिखाई गई उनका नाम पड़ा ‘टीकाकार’ और आज भी बंगाल व उड़ीसा में ‘टीकाकार’ नाम से कई परिवार पाये जाते हैं, जो मूलतः सुनार या नाई, दोनों जातियों से हो सकते हैं। शायद उनके वंशज नहीं जानते थे कि यह नाम उनके हिस्से में कहाँ से आया।
हमारे पुराने सारे कर्मकाण्डों में यह पाया जाता है कि एक छोटी सी शास्त्रीय घटना को केन्द्र में रखकर ऊपर से उत्सवों का और कर्मकाण्डों का भारी भरकम चोला पहनाया जाता था। वह चोला दिखाई पड़ता था, उसमें चमक-दमक होती थी। लोग उसे देखते, उन कर्मकाण्डों को करते और सदियों तक याद रखते। आज भी रखते हैं, लेकिन प्रायः उनकी आत्मा, अर्थात् वह छोटा सा शास्त्रीय काम जिसके लिए यह सारा ताम झाम किया गया, काल के बहाव में लुप्त हो जाता, क्योंकि उसके जानकार लोग कम रह जाते थे। आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र में रिवाज है कि चैत्र मास में छोटे-छोटे बच्चे, सिर पर तांबे का कलश लेकर नदी में नहाने जाते हैं। कलश को नीम के पत्तों से सजाया जाता है। गीले बदन नदी से देवी के मंदिर तक आकर कलश का पानी कुछ शीतला देवी पर चढ़ाते हैं और कुछ अपने सिर पर उड़ेलते हैं। इसी प्रकार शीतला सप्तमी का व्रत भी प्रसिद्ध है जो श्रावण मास में किया जाता है।
आरंभ से आयुर्वेद के प्रचार – प्रसार में विकेन्द्रीकरण का बड़ा महत्व रखा गया था जो आधुनिक केन्द्रीकरण और अस्पताल व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। आयुर्वेद के विभिन्न सिद्धान्तों को अत्यन्त छोटे छोटे कर्मकाण्डों और रीति रिवाजों में बाँटकर घर – घर तक पहुँचाया गया था। उन सिद्धान्तों के अनुपालन में परिवार की महिला सदस्योंका विशेष स्थान था। इसलिए आयुर्वेद का ज्ञान महिलाओं के पास सुरक्षित रहता था और प्रायः उन्हीं के द्वारा उपयोग में लाया जाता। महिलाओं को परिवार में सम्मान का स्थान मिलने के जो कई कारण थे उसमें स्वास्थ्य रक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारण था। यह आयुर्वेद का ज्ञान महिलाओं द्वारा परिवार के पास – पड़ोस की सेवा के लिये लगाया जाता। यदि कोई परिवार आर्थिक अड़चन में आए तभी यह ज्ञान परिवार के पुरुषों के माध्यम से आर्थिक आय जुटाने के काम में प्रयुक्त किया जाता।
चेचक या मसूरिका रोगों के विषय में चरक या सुश्रुत संहिता में अत्यन्त कम वर्णन पाया जाता है जिससे प्रतीत होता है कि पांचवीं सदी में इस रोग की भयावहता अधिक नहीं थी। किन्तु आठवीं सदी के प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रन्थ ‘माधव निदान’ में इसका विस्तृत वर्णन है। एक बार रोग हो जाये तो इसकी कोई दवा नहीं थी, केवल परहेज पर ही ज़ोर दिया जाता था। माँस-मछली, दूध, तेल, घी और मसाले कुपथ्य माने जाते थे। केला, गन्ना, पके हुए चावल, भंग, तरबूजे आदि पथ्यकर थे। बीमारी की पहचान के बाद वैद्य, ब्राम्हणों या कविराज की कोई जरूरत नहीं रहती क्योंकि दवाई तो कोई होती नहीं थी। शीतला माता के मंदिरों के पुजारी प्रायः माली समाज से या बंगाल में मालाकार समाज से होते थे। बीमारों की परिचर्या के लिए उन्हीं को बुलाया जाता था ‘माली’ आने के बाद वह घर में सारे माँसाहारी खाने बंद करवाता था। घी, तेल व मसाले भी बंद करवाये जाते। मरीज की कलाई में कुछ कौड़ियाँ, कुछ हल्दी के टुकड़े और सोने का कोई गहना बांधा जाता था। उसे केले के पत्ते पर सुलाया जाता और केवल दूध का आहार दिया जाता। उसे नीम के पत्तों से हवा की जाती। उसके कमरे में प्रवेश करने वाले को नहा धोकर आना पड़ता। शीतला माता की पंचधातु की मूर्ति का अभिषेक कर वही चरणोदक बीमार को पिलाया जाता।
रात भर शीतला माता के गीत गाये जाते। लेखक ओर्नोल्ड ने एक पूरे गीत का अंग्रेजी अनुवाद भी किया है, जो माता की प्रार्थना के लिये गाया जाता था। दानों की जलन कम करने के लिए शरीर पर पिसी हुई हल्दी, मसूर दाल का आटा या शंख भस्म का लेप किया जाता। सात दिनों तक कलश पूजा भी होती जिसमें चावल की खीर, नारियल, नीम के पत्ते इत्यादि का भोग लगता। चेचक के दाने पक चुकने के बाद, जलन को कम करने की आवश्यकता होने पर किसी तेज कांटे से उन्हें फोड़कर मवाद निकाल दिया जाता। इसके बाद के एक सप्ताह तक बीमार व्यक्ति की हर इच्छा को माता की इच्छा मानकर पूरा किया जाता और माता को ससम्मान विदा किया जाता।”
लेखक के अनुसार शीतला माता का एक बड़ा मंदिर गुडगाँव (आज का गुरुग्राम) में था जिसमें बड़ी यात्रा लगती थी। लेकिन पूरे उत्तरी भारत, राजस्थान, बिहार, बंगाल व उड़ीसा में छोटे-छोटे मंदिर थे, जहाँ चैत्र मास में शीतला माता के पर्व के लिये यात्राएं और मेले लगते थे। बंगाल और पंजाब के कई मुस्लिम परिवारों में भी शीतला माता की पूजा का रिवाज था जिसे समाप्त करने के लिए फराइजी मुस्लिम संगठन के कार्यकर्ता कोशिश किया करते।
लेखक के अनुसार बीमारी न होने का उपाय करना ब्राह्मणों के जिम्मे था जो कि गांव गांव जाकर टीके लगवाते थे। बंगाल व उड़ीसा में आज भी टीकाकार नामके कई परिवार हैं। इस विधि का भारत में काफी प्रचार था। लेकिन बीमारी हो जाने पर रोगी की व्यवस्था देखने का काम मालियों के जिम्मे था।
इस प्रकार हम देखते हैं कि इम्युनाझेशनके लिये बीमार व्यक्ति को ही साधन बनाने का सिद्धान्त और चेचक जैसी बीमारी में टीका लगाने का विधान भारत में उपजा था। तेरहवीं से अठारवीं सदी तक यह उत्तरी भारत के सभी हिस्सों में प्रचलित था। 1767 में डॉ. हॉलवेल ने भारतीय टीके की पद्धति का विस्तृत ब्यौरा लंडन के कॉलेज ऑफ फिजिक्स में प्रस्तुत किया था और इसकी भारी प्रशंसा की थी। यह पद्धति इंग्लैंड में नई-नई आई थी और हॉलवेल उन्हें इसके विषय में आश्वस्त कराना चाहता था। हॉलवेल ने बताया कि टीका लगाने के लिये भारतीय टीकाकार पिछले वर्ष के मवाद का उपयोग करते थे, नये का नहीं। साथ ही यह मवाद उसी बच्चे से लिया जाता, जिसे टीके के द्वारा शीतला के दाने दिलवाये गये हों अर्थात जिसका कण्ट्रोल्ड एनवायर्नमेंट रहा हो। टीका लगाने से पहले रुई में स्थित दवाई को गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया जाता था। बच्चों के घर और पास पड़ोस के पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाता था। बूढ़े व्यक्ति या गर्भवती महिलाओं को अलग घरों में रखा जाता ताकि उन तक बीमारी का संसर्ग न फैले। हॉलवेल के मुताबिक इस पूरे कार्यक्रम में न तो किसी बच्चे को तीव्र बीमारी होती और न ही उसका संसर्ग अन्य व्यक्तियों तक पहुँचता – यह पूर्णतया सुरक्षित कार्यक्रम था।
सन् 1839 में राधाकान्त देव (1783 – 1868) ने भी इस टीके की पद्धति का विस्तृत ब्यौरा देने वाली पुस्तक लिखी है। आरनॉल्ड कहता है – ”हालॉकि हॉलवेल या डॉ. देव यह नहीं लिख पाये कि टीका देने की यह पद्धति समाज में कितनी गहराई तक उतरी थी, लेकिन 1848 से 1867 के दौरान बंगाल के सभी जेलों के आँकड़े बताते हैं कि करीब अस्सी प्रतिशत कैदी भारतीय विधान से टीका लगवा चुके थे। असम, बंगाल, बिहार और ओरिसा में कम से कम साठ प्रतिशत लोक टीके लगवाते थे। आरनॉल्डने वर्णन किया है कि बंगाल प्रेसिडेन्सी में 1870 के दशक में चेचक से संबंधित कई जनगणनाएँ कराई गईं। ऐसी ही एक गणना 1872-73 में हुई, उसमें 17697 लोगों की गणना में पाया गया कि करीब 66 प्रतिशत लोग देसी विधान के टीके लगवा चुके थे, 5 प्रतिशत का Vaccination कराया गया था, 18 प्रतिशत को चेचक निकल चुका था और अन्य 11 प्रतिशत को अभी तक कोई सुरक्षा बहाल नहीं की गई थी।
बंगाल प्रेसिडेन्सी के बाहर काशी, कुमाँऊ, पंजाब, रावलपिण्डी, राजस्थान, सिंध, कच्छ, गुजरात और महाराष् ट्रके कोंकण प्रान् तमें भी यह विधान प्रचलित था। लेकिन दिल्ली, अवध, नेपाल, हैदराबाद और मेसूर में इसके चलन का कोई संकेत लेखक को नहीं मिल पाया। मद्रास प्रेसिडेन्सी के कुछ इलाकों में ओरिया ब्राह्मणों द्वारा टीके लगवाये जाते थे। टीके लगवाने के लिये अच्छी खासी फीस मिल जाती। लेकिन कई इलाकों में औरतों को टीका लगाने पर केवल आधी फीस मिलती थी।
राधाकान्त देव के अनुसार टीका लगाने का काम ब्राह्मणों के अलावा, आचार्य, देबांग (ज्योतिषी), कुम्हार, सांकरिया (शंख वाले) तथा नाई जमात के लोग भी करते थे। बंगाल में माली समाज के लोग और बालासोर में मस्तान समाज के, तो बिहार में पछानिया समाज के लोग, मुस्लिमों में बुनकर और सिंदूरिये वर्ग के लोग टीका लगाते थे। कोंकण में कुनबी समाज तो गोवा में कॅथोलिक चर्चों के पादरी भी टीका लगाते थे। टीका लगाने के महीनों में, अर्थात् फाल्गुन, चैत्र, बैसाख में हर महीने सौ – सवा सौ रुपये की कमाई हो जाती, जो उस जमाने में अच्छी खासी सम्पत्ति थी। कई गाँवों का अपना खास टीका लगवाने वाला होता था और कई परिवारों में यह पुश्तैनी कला चली आई थी। लेखक के मुताबिक ‘चूँकि टीका लगवाने की यह विधि ब्रिटेन में भी धीरे-धीरे मान्य हो रही थी, अतः बंगाल के कई अंग्रेज परिवार भी टीके लगवाने लगे थे। लेकिन सन् 1798 में सर जेनर ने गाय के थन पर निकले चेचक के दानों से Vaccine बनाने की विधि ढूँढ़ी तो इंग्लैंड में उसका भारी स्वागत हुआ।‘अब उस जादू टोने वाले देश के टीके की बजाय हम अपने डॉक्टर की विधि का प्रयोग करेंगे’। जैसे ही जेनर की विधि हाथ में आई, अंग्रेजों ने मान लिया कि इसके सिवा जो भी विधि जहाँ भी हो, वह बकवास है और उसे रोकना पड़ेगा।
जेनर की विधि सबसे पहले 1802 में मुंबई में लाई गई और 1804 में बंगाल में। इसके बाद ब्रिटिश शासन ने हर तरह से प्रयास किया कि भारतीयों की टीका लगाने की विधि अर्थात् Variolation को समाप्त किया जाए। इसका सबसे अच्छा उपाय यह था कि Variolation के द्वारा टीका लगवाने को गुनाह करार दिया गया और टीका लगवाने वालों को जेल भेजा गया। करीब 1830 के बाद चेचक के विषय में अंग्रेजों के द्वारा लिखित जितने भी ब्यौरे मिलेंगे उनमें Variolation की विधि को बकवास बताया गया है और भारतीयों की तथा उनकी अंधश्रद्धा की भरपूर निन्दा की गई। ‘वे (भारतीय) जेनर साहब के Vaccination जैसे अनमोल रत् नको ठुकरा रहे थे, जो उन्हें अंग्रेज डॉक्टरों की दया से मिल रहा था और जिसके प्रति कृतज्ञता दर्शाना भारतीयों का कर्तव्य था।’ भारतीयों द्वारा देसी पद्धति से टीका लगवाने को ‘मृत्यु का व्यापार’ या “Murderous trade” कहा गया।
”वैक्सीनेशन को भारतीयों ने शीघ्रता से सिर आँखों पर नहीं लिया इससे कई अंग्रेज अफसर रुष्ट थे। शूलब्रेड ने उन्हें मूर्ख, अज्ञानी और हर नये अविष्कार का शत्रु कहा (1804) तो डंकन स्टेवार्ट ने अकृतज्ञ और मूढ़ कहा (1840) जबकि 1878 में कलकत्ता के सॅनिटरी कमिश्नर ने उन्हें अंधविश्वासी, रूढ़िवादी और जातीयवादी कहा। भारतीयों की टीका पद्धति को ही इस व्यवहार का कारण माना गया और कहा गया कि सारे भारतीय टीकाकार अपनी रोजी रोटी छिन जाने के डर से वैक्सीनेशन के बारे में गलत बातें फैला रहे थे, जबकि भारतीय पद्धति में ही अधिक लोग मरते हैं.” — आरनॉल्ड
”खुद नियति ने यह विधान किया कि हम इस देश पर राज करें और यहाँ लाखों करोड़ों मूढ़ और अज्ञानी प्रजाजनों को उस आत्मक्लेश से बचायें जिसके कारण वे भारतीय टीका लगवाते हैं” – शूलब्रेड
लेकिन शूलब्रेड के ही समकालीन बुचानन ने इस पद्धति में कई अच्छाइयों का वर्णन किया है और 1860 में कलकत्ता के वैक्सीनेशन के सुपरिटेंडेंट जनरल चार्लस् ने लिखा है ”यदि सारे विधि विधानों का ठीक से पालन हो तो भारतीय पद्धति में चेचक की महामारी फैलने की कोई संभावना नहीं है, हालाँकि मैं स्वयं वैक्सिनेशनको बेहतर समझता हूँ फिर भी मेरा सुझाव है कि भारतीय टीकादारों पर पाबन्दी लगाने के बजाय उनका रजिस्ट्रेशन करके उन्हें उनकी अपनी प्रणाली से टीके लगाने दिये जायें।” जाहिर है कि यह सुझाव अंग्रेजी हुकूमत को पसंद नहीं आया।
अंग्रेजी पद्धति के लोकप्रिय न होने का एक कारण यह भी था कि काफी वर्षों तक अंग्रेजी पद्धति में कई कठिनाईयाँ रही थीं। उन्नींसवीं सदी के अंत तक यह पद्धति काफी क्लेशकारक भी थी। भारतवर्ष में गायों को चेचक की बीमारी नहीं होती थी। अतः गाय के चेचक का मवाद (जिसे वैक्सिन कहा गया) इंग्लैंड से लाया जाता था फिर बगदाद से बंबई तक इसे बच्चों की श्रृखंला के द्वारा लाया जाता था – अर्थात् किसी बच्चे को गाय के वैक्सीन से टीका लगा कर उसे होने वाली जख् मके पकने पर उसमें से मवाद निकालकर अगले बच्चे को टीका लगाया जाता था।”
बाद में गाय के वैक्सीन को शीशी में बन्द करके भेजा जाने लगा। परंतु गर्मी से या देर से पहुँचने पर उसका प्रभाव नष्ट हो जाता था। उसके कारण बड़े बड़े नासूर भी पैदा होते थे। गर्मियों में दिये जाने वाले टीके कारगर नहीं थे, अतएव छह महीनों के बाद टीके बंद करने पड़ते थे और अगले वर्ष फिर से बच्चों की श्रृखंला बनाकर ही टीके का वैक्सीन भारत में लाया जा सकता था। यूरोप और भारत में कुछ लोगों ने इसे बच्चों के प्रति अन्याय बताया और यह भी माना जाता था कि इसी पद्धति के कारण सिफिलस या कुष्ठ रोग भी फैलते हैं।
सन् 1850 में बम्बई में वैक्सीनेशन डिविजन ने गाय के बछड़ों में वैक्सिनेशन कर उनके मवाद से टीके बनाने का प्रयास किया परंतु यह खर्चीला उपाय था।
सन् 1893 में बंगाल के सॅनिटरी कमिश्नर डायसन ने लिखा है – अंग्रेजी पद्धति में एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीका दिया जाता था। जिस बच्चे का घाव पक गया हो उसे दूसरे गाँवों में ले जाकर उसके घावों का मवाद निकालकर अन्य बच्चों को टीका लगाया जाता। कई बार घाव को जोर से दबा-दबाकर मवाद निकाला जाता ताकि अधिक बच्चों को टीका लगाया जा सके। बच्चे, उनकी माएं और अन्य परिवारवाले रोते तड़पते थे। टीका लगवाने वाले परिवार भी रोते क्योंकि उनके बच्चों को भी आगे इसी तरह से प्रयुक्त किया जाता था। गांव वाले मानते थे कि इन अंग्रेज टीकादारों से बचने का एक ही रास्ता था – कि उन्हें चाँदी के सिक्के दिये जायें। यह सही है कि इस विधि में बच्चे को कोई बीमारी नहीं होती थी या उसे चेचक के दाने नहीं निकलते थे, जबकि भारतीय पद्धति में पचास से सौ तक दाने निकल आते थे फिर भी कुल मिलाकर भारतीय पद्धति में तकलीफें कम थीं। जो भी थीं उन्हे शीतला माता की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया जाता था।
इस सारे विवरण को विस्तार से पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि जब अर्नोल्ड जैसा ब्रिटिश व्यक्ति, भारतीय चिकित्सा पद्धति पर इतना अध्ययन कर के यह पुस्तक लिखता है तो अंग्रेजों ने उस पर विचार क्यों नहीं किया…? इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है, कि अंग्रेजों का महिमामंडन करने के लिए उन्हें ‘गुणग्राहक’ जैसे विशेषणों से नवाजा जाता है जो गलत है। अंग्रेज़ तो पक्के व्यापारी थे। उन्हें प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के गुण – दोषों से कुछ लेना देना नहीं था। उन्हें तो मात्र, उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन, उनके द्वारा बनाई गई औषधियां, भारत के घर घर तक पहुंचानी थीं। इसीलिए अंग्रेजों ने एक अत्यंत सुव्यवस्थित चिकित्सा पध्दति को, ज़ोर-ज़बरदस्ती कर के समाप्त किया।
अंग्रेजों के भारत से निकालने के समय, बहुत कम आयुर्वेदिक दवाखाने और वैद्य बचे थे। अंग्रेजों ने, सारे देश में अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के दवाखाने, अस्पताल और डॉक्टर्स बनाकर, इस देश की प्राचीन और उन्नत चिकित्सा पद्धति को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया !
संदर्भ –
1. Colonizing the Body : State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth Century India – David Arnold (August 1993)
2. Medical History of British India
3. Public Health in British India : A Brief Account of the History of Medical Services and Disease Prevention in Colonial India – Muhammad Umair Mushtaq (January 2009)
4. War Against Smallpox – Michael Bennet
5. The Anarchy – William Darymple
6. An Era of Darkness – Shashi Tharoor
7. १८ वी शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तंत्रज्ञान – धरमपाल
8. Medical Encounters in British India – Deepak Kumar and Raj Sekhar Basu
9. The British in India – David Gilmour
10. The Social History of Health and Medicine in Colonial India – Biswamoy Pati and Mark Harrison