हम बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की अंतहीन भीड़ में तो नहीं धकेल रहे?
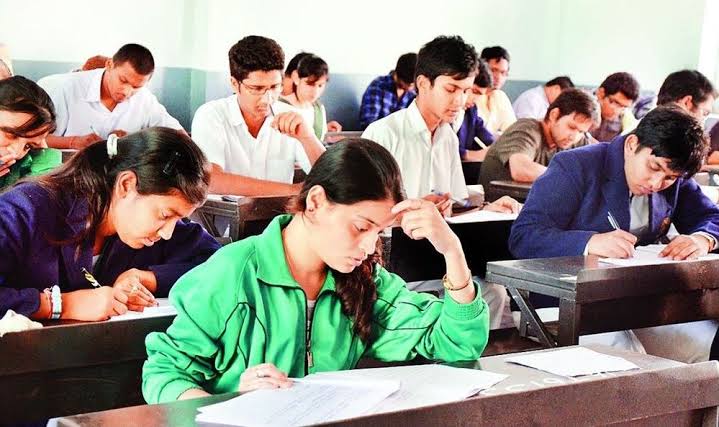
प्रणय कुमार
अंकों की प्रतिस्पर्धा का आत्मघाती दबाव दारुण और दुःखद है। इस दबाव में बच्चे सहयोगी बनने की अपेक्षा परस्पर प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं। बच्चे माता-पिता की अंतहीन महत्वाकांक्षाओं को ढोते-ढोते अपना सहज-स्वाभाविक जीवन भूल रहे हैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि उन्हें उनके स्वाभाविक स्वरूप के विपरीत भेड़चाल के कारण हम कहीं उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की अंतहीन भीड़ में तो नहीं धकेल रहे हैं?
बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो गये हैं। इन परीक्षा के परिणामों से छात्रों के साथ-साथ अभिभावक भी प्रभावित होते हैं। यह स्वभाविक भी है। लेकिन क्या कभी हमने इसके दूसरे पहलू पर विचार किया है? इन परीक्षाओं के दबाव और तनाव में एक ओर गुम होता बचपन तो दूसरी ओर येन-केन-प्रकारेण पास होने और अधिक-से-अधिक अंक लाने का तीव्रतम उतावलापन दृष्टिगोचर होता है। और इसके साथ वही पुराना सवाल कि क्या कागज के एक टुकड़े भर से किसी के ज्ञान या व्यक्तित्व का समग्र और सतत आंकलन-मूल्यांकन किया जा सकता है? क्या किसी एक परीक्षा की सफलता-असफलता पर ही भविष्य की सारी सफलताएँ निर्भर किया करती हैं? जीवन की वास्तविक परीक्षाओं में ये परीक्षाएँ कितनी सहायक हैं? यह जाने-विचारे बिना हम सब अंकों के पीछे बदहवास होकर दौड़ लगा रहे हैं। कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ जाकर रुकेंगे, पता नहीं? क्या व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं एवं विशेषताओं का कोई अर्थ नहीं?
समाज में जिसे सफल माना समझा जाता है, वह कितना सुखी शांत समझदार जिम्मेदार संवेदनशील व सरोकारधर्मी है? क्या इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं? वर्तमान शिक्षा की दशा और दिशा के लिए उत्तरदायी मैकॉले से पूर्व लौटना तो संभव नहीं, कदाचित यह उचित भी नहीं। समय प्रगति और परिवर्तन का स्वाभाविक वाहक होता है। पर क्या कदम-ताल को ही प्रगति एवं परिवर्तन का पर्याय माना जा सकता है? अंकों की अंधी दौड़ का हिस्सा बनने से उचित क्या यह नहीं होता कि हम इस पर गंभीर चिंतन और व्यापक विमर्श करते कि क्यों हमारे शिक्षण-संस्थान वैश्विक मानकों एवं गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते? क्यों हमारे शिक्षण-संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में मौलिक शोधों एवं वैज्ञानिक-व्यावहारिक दृष्टिकोण का अभाव परिलक्षित होता है? क्यों हमारे शिक्षण-संस्थान अभिनव प्रयोगों, नवोन्मेषी पद्धतियों, विश्लेषणपरक प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देते? क्यों हमारे शिक्षण-संस्थानों से निकले अधिकांश विद्यार्थी आत्मनिर्भर और स्वावलंबी नहीं बन पाते? क्यों वे साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों, विषमताओं, प्रतिकूलताओं का सामना नहीं कर पाते? यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत कम हैं, पर वह नैतिक-साहित्यिक- सामाजिक-सांस्कृतिक संस्कारों और सरोकारों का धनी है तो क्या यह उसकी योग्यता का मापदंड नहीं होना चाहिए?
अंकों की प्रतिस्पर्धा का आत्मघाती दबाव दारुण और दुःखद है। इस दबाव में बच्चे सहयोगी बनने की अपेक्षा परस्पर प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं। यह अंधी प्रतिस्पर्धा उन्हें अंतहीन कुंठा की ओर ले जा रही है। और यह तथ्य है कि प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में व्यक्ति प्रकृति में सर्वत्र व्याप्त सहयोग, सामंजस्य और सौंदर्य को विस्मृत कर बैठता है। फिर वह चराचर में फैले जीवन के गीत को गुनगुनाना, गाना और सुनना ही भूल जाता है। प्रतिस्पर्धा करते-करते वह अपने घर-परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति भी प्रतिस्पर्धी-भाव रखने लगता है। कई बार तो वह अपनों के प्रति भी कटु और कृतघ्न हो उठता है। यह कैसा दुर्भाग्य है कि हम उसे बचपन से ही दूसरों को पछाड़ने की सीख दे रहे हैं। जबकि हमें साथ, सहयोग और सामंजस्य की सीख देनी चाहिए। जीवन एक संघर्ष है उससे कहीं अधिक आवश्यक है यह जानना-समझना कि जीवन एक समन्वय है।
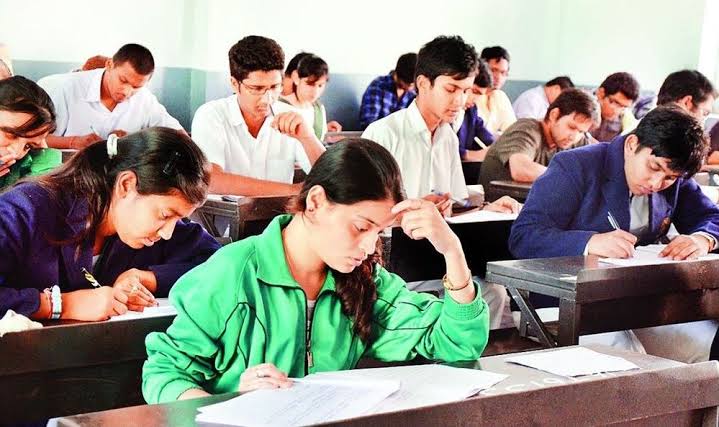
कुछ विद्यालय-महाविद्यालय, शिक्षण-संस्थान प्रयोगधर्मिता और समग्रता को लेकर चलना भी चाहते हैं, पर उन्हें समाज का व्यापक समर्थन और सहयोग नहीं मिल पाता। रातों-रात करोड़पति बनने या छा जाने की मानसिकता हमारी सोचने -समझने की शक्ति को कुंद करती है। सफलता के सब्ज़बाग दिखाते और सपने बेचते ग्राम-नगर-गली मुहल्ले में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए कोचिंग संस्थान कोढ़ में खाज़ की तरह हैं। वे सफलता का सौदा करते हैं। सफल अभ्यर्थियों के चमकते-दमकते सितारा चेहरों और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए अतिरेकी दावों के पीछे, हमें विफल अभ्यर्थियों की अंतहीन सूची और उनका दर्द दिखायी नहीं देता। सजे-चमचमाते कालीन के पीछे के स्याह-कटु सत्य को कौन देखे-दिखाये?
भ्रामक प्रचार-प्रसार या आक्रामक विज्ञापनों के जरिये भोले-भाले मासूमों और उनके लिए अपने पलकों की कोरों में सपने सजाए तमाम अभिभावकों को बहलाया-फुसलाया जाता है। बल्कि कई बार तो बहुतेरे अभिभावक अपने बच्चों की क्षमता और रुचि का विचार किए बिना अपने सपनों व महत्वाकांक्षाओं का बोझ जाने-अनजाने अपने बच्चों के कच्चे-कमज़ोर कंधों पर डालने की भूल कर बैठते हैं। प्रायः बच्चे उनके सपनों व महत्त्वाकांक्षाओं का भार ढोते-ढोते अपना सहज-स्वाभाविक बचपन और जीवन तक भूल जाते हैं। वे कुछ और कर सकते थे। कुछ बेहतर बन सकते थे! लेकिन भेड़चाल के कारण हमने उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं (जेईई, नीट, क्लेट, सीए) की अंतहीन भीड़ में धकेल दिया जाता है! और यदि वे सफल हुए तो ठीक, पर कहीं जो वे विफल हुए तो जीवन भर वे उस विफलता की ग्लानि भरी मनोदशा से बाहर नहीं निकल पाते ! फिर उनके होठों से सहज हास और जीवन से सहज आनंद एवं उत्साह ग़ायब हो जाता है। केवल आस-पड़ोस को देखकर कहीं हम अपने बच्चों से अपने परवरिश की क़ीमत वसूलने की भूल तो नहीं कर रहे हैं?
समाज और संस्थाओं को सोचना होगा कि ये बच्चे या विद्यार्थी उत्पाद न होकर जीते-जागते मनुष्य हैं। और मनुष्य का निर्माण स्नेह-समर्पण-त्याग-संयम-धैर्य-सहयोग-समझ और संवेदनाओं से ही संभव है। ध्यान रहे कि मनुष्य का मनुष्य हो जाना ही उसकी चरम उपलब्धि है। इसलिए अपनी संततियों को अंकों की अंधी प्रतिस्पर्द्धा एवं अंतहीन दौड़ में झोंकने की बजाय हमें उनके समग्र, संतुलित एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जीवन बहुरंगी एवं बहुपक्षीय है और हर रंग व पक्ष का अपना सौंदर्य और महत्त्व है।
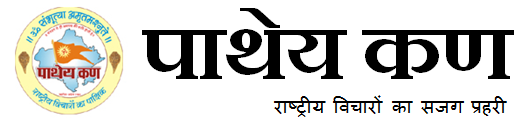
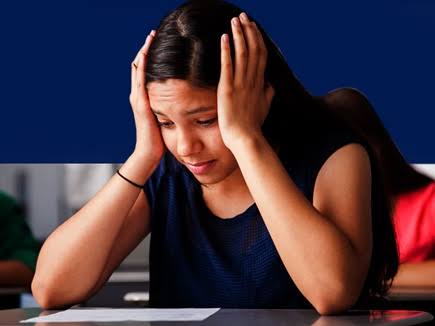
बहुत उपयोगी आलेख। विचारोत्तेजक।
धन्यवाद।
आनंद कुमार
पाथेय कण एक बेहतरीन पोर्टल है। इसके आलेख बहुत विचारोत्तेजक ज्ञानवर्धक होते हैं। आज के समय में होटल के सभी आलेख बहुत सामयिक और रुचिकर हैं
प्रशंसा गुप्ता